आधुनिक भारत के इतिहास में, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने साथ पीड़ा और गर्व दोनों लाया। उसके अनेकों मोड़ से गुज़र से एक नया भारत उभरा। अब हम पढ़ेंगे (१) १८५७ का विद्रोह, (२) १८५७ पश्चात भारत, (३) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में
FREE PT APP | CURRENT AFFAIRS Home All Posts Shrutis Power of 10 | CIVILS TAPASYA Home Tapasya Annual Prep - TAP GS-Study Mat. Exams Analyses Downloads | APTITUDE Power of Apti | TEST SERIES | CONTRIBUTE | TESTIMONIALS | PREMIUM PT GURUKUL | PRABODHAN Mastercourse | C.S.E. Self-Prep Online | SANDEEP SIR Site Youtube
A. १८५७ का विद्रोह (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम)
A.1 प्रस्तावना
वह पहला स्थानीय विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश शासन हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया इसे अलग-अलग इतिहासकारों ने अनेक नामों से वर्णित किया है (अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार)। इनमें 'सिपाही विद्रोह', 'महान विद्रोह' और '1857 का विद्रोह' शामिल हैं। अधिकांश भारतीय इसे ‘प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' कहना पसंद करते हैं। निःसंदेह यह ब्रिटिश साम्राज्य की कई दशकों की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय जन भावना का प्रस्फुटन था। विद्रोह तक, ब्रिटिश कई दंगे और कबीलाई लड़ाईयों को दबाने में सफल हुए थे, या 1857 के ग्रीष्म माह तक उनको कुछ सुविधाएँ या छूट देकर सफल रहे थे। यह संघर्ष वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
A.2 कारण
हालाँकि 1857 के भारतीय विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा प्रयोग किये गए हथियारों में एक छोटा सा परिवर्तन था, इसके कई अन्य धार्मिक और आर्थिक कारण थे जिनके कारण यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई पद्धति की 1853 एनफील्ड राइफल में उन्नयन किया था, जिसमें चर्बीयुक्त कागज़ कारतूसों का उपयोग किया जाता था। कारतूसों को खोलने के लिए और उन्हें राइफल में भरने के लिए सिपाहियों को कागज को चबाना पड़ता था, और उसे अपने दांतों से फाड़ना पड़ता था।
1856 में इस प्रकार की अफवाहें फैलना शुरू हुईं कि कारतूसों पर लगी हुई चर्बी गौमांस वसा और सूअर के मांस की चर्बी के मिश्रण से बनी हुई थी; निश्चित ही हिंदू धर्म में गौमांस का सेवन निषिद्ध है, जबकि सूअर के मांस का सेवन इस्लाम के अनुसार हराम है। इस प्रकार, इस छोटे से परिवर्तन से ब्रिटिशों ने हिंदू और मुस्लिम, दोनों सैनिकों को गंभीर रूप से आहत कर दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। ब्रिटिशों की ‘कालातीत सिद्धांत’ (विलय सिद्धांत / Doctrine of Lapse) नीति के अनुसार गोद लिए हुए बच्चे सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के लिए अपात्र थे। इस सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिशों ने अनेक रियासतों का विलय कर लिया था। यह अनेक रियासतों में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने का एक प्रयास था, जो ब्रिटिश सत्ता से नाममात्र के लिए स्वतंत्र थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की जमीन बडे़ पैमाने पर जब्त की थी, और उसे किसानों को वितरित कर दिया था। हालांकि उन्होंने किसान समुदाय पर भारी कर भी अधिरोपित कर दिए थे। इसके कारण किसान और जमींदार दोनों नाराज थे। अवध विशेष रूप से अस्थिर था क्योंकि अवध से बड़ी संख्या में सिपाही ब्रिटिश सेना में थे, और इसने उनके परिवारों को सीधे प्रभावित किया।
- [col]
- ब्रिटिशों के सुधारवादी उत्साह ने भी संकट को भड़काने में और अधिक योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं को प्रतिबंधित कर दिया, जिनमें सती प्रथा या विधवाओं को पति की चिता के साथ जलाना शामिल था, इसके कारण अनेक हिंदुओं का गुस्सा उबल रहा था। कंपनी ने जाति व्यवस्था को भी कमजोर करने का प्रयास किया, जो प्रबोधन के बाद की ब्रिटिश संवेदनाओं को अन्यायपूर्ण प्रतीत हो रही थी। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश अधिकारियों और धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का उपदेश देना शुरू किया, साथ ही धर्म परिवर्तन भी शुरू हो गया थे। भारतीयों को लगने लगा, और यह तार्किक भी था, कि हमारे धर्मों पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आक्रमण किया जा रहा था।
- अंततः सभी जातियों और धर्मों के भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के दमन और उनके द्वारा किये जाने वाले अपमान की अनुभूति होने लगी। कंपनी के जो अधिकारी भारतीयों को गलियां देते थे या उनकी हत्या भी कर देते थे, उन्हें षायद ही उचित सजा मिलती थी; यदि उनपर मुकदमे चलाये भी जाते थे, तो भी उन्हें दोषी करार दिया जाना दुर्लभ था, और जो अपील करने में सक्षम थे, वे लगभग अनिश्चित समय तक अपील करते रहते थे। ब्रिटिशों के बीच जातीय श्रेष्ठत्व की सामान्य भावना ने देशभर के भारतीयों को आक्रोशित कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां भी व्यापक और प्रचलित असंतोष का कारण बन गई थीं।
- किसान उच्च राजस्व की मांग और राजस्व संग्रहण की कठोर नीति के कारण व्यथित थे। शिल्पकार और कारीगर भारत में आयात होने वाले सस्ते ब्रिटिश विनिर्मित माल के कारण तबाह हो गए थे, जिसके कारण उनके हाथ से बने सामान निर्माण की दृष्टि से भी महंगे हो गए थे। जो लोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करके उदर निर्वाह करते थे उनका निर्वाह का स्रोत ही नष्ट हो गया था क्योंकि पुराने शासक वर्ग के प्रतिस्थापित होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाला राजाश्रय समाप्त हो चुका था। भ्रष्ट और अनुत्तरदायी प्रशासन ने लोगों के दुखों में और अधिक वृद्धि की थी।
अतः सारे कारकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैंः
- [message]
- अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक उत्पीड़न
- अंग्रेज़ों भू-राजस्व नीति और कानून व्यवस्था एवं प्रशासन
- भारतीय इतिहास पर श्रेष्ठता की ब्रिटिश प्रवृत्ति
- क्षेत्रों पर अधिकार करने की ब्रिटिश नीति - अवध का अधिग्रहण और विलय की नीति ने प्रांतीय शासकों को नाराज कर दिया
- विद्रोह का तात्कालिक कारण सेना की बदतर स्थिति के कारण उनमें उत्पन्न अंसतोष था
- इनफील्ड राइफल को शामिल करना जिसके कारतूसों में स्नेहक आवरण था जो जानवरों के मांस से बना था (हिंदू और मुसलमान दोनों आहत थे क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं)
- ईसाई धर्म के प्रसार का भय
A.3 विद्रोह की शुरुआत
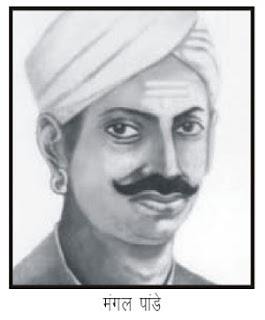 29 मार्च 1857 को 34 रेजीमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड़ के दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। मौजूद भारतीय सिपाहियों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई।
29 मार्च 1857 को 34 रेजीमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड़ के दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। मौजूद भारतीय सिपाहियों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई।
यह खबर जंगल की आग की तरह देश की सभी छावनियों में फैल गई और जल्द ही देशव्यापी सिपाही विद्रोह लखनऊ, अम्बाला, बहरामपुर और मेरठ में फैल गया।
10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। नागरिकों के साथ सैनिकों ने एक क्रोधोन्मन नारा लगाया-मारो फिरंगी को। उन्होंने जेल तोड़ दी यूरोपीय महिला और पुरुषों को मार डाला उनके घरों को जला दिया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। अगली सुबह दिल्ली में मार्च करते सैनिकों की उपस्थिति स्थानीय सैनिकों के लिए एक संकेत थी। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया शहर पर कब्जा कर लिया और 80 वर्षीय वृद्ध बहादुरशाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
दिल्ली पर कब्जा करने के एक महीने के भीतर विद्रोह देश के अन्य भागों में भी फैल गया जैसे - कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। किसी भी नेता के न होने के कारण विद्रोही भारतीय समाज के पारंपरिक नेताओं के पास गए। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजी राव 11 के दत्तक पुत्र-नाना साहेब ने सैनिकों का नेतृत्व किया। झाँसी में रानी लक्ष्मी बाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बरेली में खान बहादुर अन्य नेतृत्वकर्ता थे। यद्यपि ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक सामान्य घृणा के अलावा विद्रोहियों का कोई राजनीतिक विचार या भविष्य के लिए कोई निश्चित दृष्टि नहीं थी। वे सभी अपने अतीत के कैदी थे और प्रमुखतः अपनी खोई सुविधाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं कि वे नए राजनीतिक क्रम को समझ पाने में असमर्थ साबित हुए। जॉन लारेंस ने सत्य कहा है कि ‘‘अगर उनमें से एक भी योग्य नेता हुआ होता तो हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके होते।’’ This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
A.4 विद्रोह का विस्तार
 1857 के विद्रोह के उत्केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी और बिहार के आरा थे। दिल्ली में नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह के पास था परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिकों के एक विचारमंच के पास था जिसका नेतृत्व सेनापति बख्त खान कर रहे थे, जिन्होंने बरेली की टुकड़ियों का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली लाये। ब्रिटिश सेना में वे केवल तोपखाने में एक सामान्य सैनिक थे। इस विचारमंच में दस सदस्य थे जिनमें से छह सदस्य सेना से थे और अन्य चार सदस्य अन्य नागरिक विभागों से थे। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। यह विचारमंच ‘‘दिल्ली की सरकार के सम्राट के नाम से‘‘ राज्य के सभी कार्य करता था। हालांकि बहादुर शाह के कमजोर व्यक्तित्व, उनकी वृद्धावस्था और नेतृत्व गुणों के अभाव ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में एक राजनीतिक दुर्बलता निर्मित की और इसके कारण इस विद्रोह को काफी क्षति हुई।
1857 के विद्रोह के उत्केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी और बिहार के आरा थे। दिल्ली में नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह के पास था परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिकों के एक विचारमंच के पास था जिसका नेतृत्व सेनापति बख्त खान कर रहे थे, जिन्होंने बरेली की टुकड़ियों का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली लाये। ब्रिटिश सेना में वे केवल तोपखाने में एक सामान्य सैनिक थे। इस विचारमंच में दस सदस्य थे जिनमें से छह सदस्य सेना से थे और अन्य चार सदस्य अन्य नागरिक विभागों से थे। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। यह विचारमंच ‘‘दिल्ली की सरकार के सम्राट के नाम से‘‘ राज्य के सभी कार्य करता था। हालांकि बहादुर शाह के कमजोर व्यक्तित्व, उनकी वृद्धावस्था और नेतृत्व गुणों के अभाव ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में एक राजनीतिक दुर्बलता निर्मित की और इसके कारण इस विद्रोह को काफी क्षति हुई।
कानपुर में बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता से ब्रिटिशों को कानपुर से बाहर कर दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उसी समय उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट स्वीकार किया और स्वयं को उनका गवर्नर घोषित किया। नाना साहिब की ओर से लड़ते हुए युद्ध की मुख्य ज़िम्मेदारी नाना साहेब के सबसे विश्वस्त सैनिकों में से एक, तात्या टोपे, के कंधों पर थी। कानपुर पर कब्जे के दौरान नाना साहिब के वफादार सैनिकों ने उस क्षेत्र में छिपी ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया। अंततः अनेक ब्रिटिश सैनिक या तो बंदी बना लिए गए या वे युद्ध में मारे गए (बाद में ये हत्याएं ब्रिटिशों के लिए दिल्ली सहित विद्रोह के अन्य केंद्रों पर बडे़ पैमाने पर नरसंहार करने का बहाना बनीं)। जब तक ब्रिटिश सेनाएं कानपुर पहुंचीं तब तक तात्या टोपे और नाना साहेब शहर छोड़ चुके थे। परंतु 1857 का विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था। तात्या टोपे ने कहीं अधिक श्रेष्ठ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अपना युद्ध जारी रखा। नवंबर 1857 आते-आते उन्होंने काफी बड़ी सेना इकठ्ठा कर ली थी, जिनमें से अनेक लोग ग्वालियर के विद्रोही थे, और कानपुर को वापस पाने का एक दुःसाहसी प्रयास किया। यह एक भीषण युद्ध था परंतु इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की विजय हुई। विद्रोह का कानपुर संस्करण इसीके साथ लगभग समाप्त हो गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
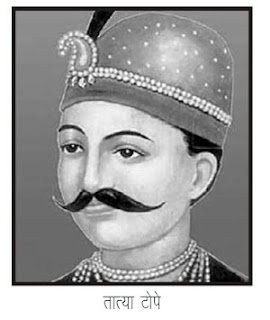 तात्या टोपे ने फिर से सेना एकत्रित की, व एक समय पर तो उन्होंने झाँसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ भी मिलाया, जिनकी अंततः युद्ध में मृत्यु हुई।
तात्या टोपे ने फिर से सेना एकत्रित की, व एक समय पर तो उन्होंने झाँसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ भी मिलाया, जिनकी अंततः युद्ध में मृत्यु हुई।
उन्होंने विभिन्न छोटे राजाओं के साथ मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला अभियान लगभग एक वर्ष तक जारी रखा। उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध बनास नदी के तट पर सांगानेर के निकट युद्ध किया और अन्य स्थानों के साथ ही छोटा उदयपुर में भी ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किया। ऐसे प्रत्येक युद्ध के बाद वे अपनी सेना का पुनर्गठन करते रहे। फिर भी उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में विद्रोह को कठोरता से कुचलने के साथ ही वह समय दूर नहीं था जब अपनी दुर्जेय सैन्य क्षमताओं के साथ ब्रिटिश तात्या टोपे सहित अंतिम विद्रोहियों को पकड़ सके। इसके अतिरिक्त तात्या टोपे की सेना बिखर चुकी थी और क्षीण हो चुकी थी। मुख्यधारा इतिहासकारों के दस्तावेजों के अनुसार अंततः एक सहयोगी द्वारा धोखा देने पर अप्रैल 1859 में उन्हें बंदी बना लिया गया, और एक छोटे सैन्य मुकदमे के बाद 18 अप्रैल को ब्रिटिशों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई।
नाना साहेब को कानपुर में पराजित किया गया। वे अंत तक दुःसाहसी बने रहे और उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया, और 1859 के प्रारंभ में छिप कर नेपाल चले गए, उसके बाद उनके बारे में फिर कोई जानकारी नहीं मिली।
लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने अपने युवा पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में सिपाहियों की सहायता से और अवध के जमींदारों और कृषकों की सहायता से बेगम ने ब्रिटिशों के विरुद्ध एक पुरज़ोर आक्रमण किया। शहर छोड़ने को मजबूर ब्रिटिशों ने स्वयं को रेज़ीडेंसी भवन में सुरक्षित रूप से बंद कर लिया। अंत में रेज़ीडेंसी का अधिग्रहण असफल हुआ, और छोटी ब्रिटिश सेना ने अनुकरणीय धैर्य और साहस के साथ युद्ध किया।
1857 के विद्रोह के महानतम सेनापतियों में से एक और संभवतः भारतीय इतिहास की महानतम नायिकाओं में से एक थी झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई।
- [col]
- 1842 में मणिकर्णिका, जो नाम उन्हें उनके माता-पिता द्वारा दिया गया था, का विवाह झाँसी के महाराजा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, और उसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों लिखा जाना था और जिसे बहुत सम्मान प्राप्त होना था। 1851 में इस युगल को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा, परंतु दुर्भाग्यवश उनके इस शिशु की मृत्यु चार महीने की आयु में ही हो गई। शिशु अवस्था में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद राजा और लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव के चचेरे भाई के आनंद राव नामक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम पुनः दामोदर राव रखा।
- इस दत्तक ग्रहण समारोह के साक्षी एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी भी थे। राजा गंगाधर राव ने इस ब्रिटिश अधिकारी को एक पात्र भी दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि झाँसी की सत्ता लक्ष्मीबाई को उनके जीवन-पर्यंत प्रदान की जाये। नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटिशों ने विलय का सिद्धान्त यह कहते हुए अनुप्रयुक्त कर दिया कि वे इस दत्तक पुत्र को राजा के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं देंगे और झाँसी का ब्रिटिश प्रदेश में विलय करेंगे।
- अपने प्रदेश के बारे में ब्रिटिशों द्वारा किये जा रहे इस पक्षपात के प्रतिक्रियास्वरुप लक्ष्मीबाई ने एक ब्रिटिश वकील की सलाह प्राप्त की और यह अनुरोध किया कि उनके मामले की सुनवाई लंदन में की जाए। इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया। ब्रिटिशों ने झाँसी के राज्य आभूषण अधिग्रहित कर लिए और 1854 में लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये का निवृत्ति वेतन प्रदान किया और उन्हें अपना महल और किला छोड़ने का आदेश दिया। वे रानी महल नामक महल में चली गईं, जिसे अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।
 महल से निष्कासित किये जाने के बाद भी लक्ष्मीबाई झाँसी की ब्रिटिश अधिग्रहण से रक्षा करने के प्रति दृढ़ थीं। लक्ष्मीबाई ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करना शुरू किया और पुरुषों और महिलाओं की एक सेना बनाई जिन्हें युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था।
महल से निष्कासित किये जाने के बाद भी लक्ष्मीबाई झाँसी की ब्रिटिश अधिग्रहण से रक्षा करने के प्रति दृढ़ थीं। लक्ष्मीबाई ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करना शुरू किया और पुरुषों और महिलाओं की एक सेना बनाई जिन्हें युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था।
उसके बाद युवा रानी ने अपनी शक्ति विद्रोहियों के साथ लगाने का निर्णय लिया, और अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए वीरतापूर्वक लडीं। उनकी वीरता, साहस और सैन्य कौशल के किस्सों ने उनके देशवासियों को आज तक प्रेरित किया है। एक भीषण युद्ध, ‘‘जिसमें महिलाऐं भी आक्रमण करती हुई और गोलाबारूद वितरित करती हुई देखी जा रहीं थीं, के बाद ब्रिटिश सेनाओं द्वारा झाँसी के बाहर खदेड़ दिए जाने के बाद रानी ने अपने अनुयाइयों को यह शपथ दिलाई कि ‘‘अपने स्वयं के हाथों से हम अपनी आजादशाही (स्वतंत्र शासन) को दफन नहीं करेंगे।‘‘ तात्या टोपे और अपने विश्वासपात्र अफगान अंगरक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों के वफादार महाराजा सिंधिया ने रानी के विरुद्ध लड़ने का प्रयास किया परंतु उनकी अधिकांश सेना रानी के साथ जा कर मिल गई। सिंधिया ने आगरा में अंग्रेज़ों की शरण ली।
16 जून 1858 को सेनापति रोज़ की सेना ने मोरार पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष के 17 जून को ग्वालियर के फूल बाग के निकट कैप्टेन हेनगे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना का सामना किया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रहीं थीं, जब वे इस क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। घुडसवार की पोशाख में पुरुष वेशभूषा में शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित, अपने नवजात पुत्र को पीठ पर बाँध कर घोडे पर सवार लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करना शुरू किया। ब्रिटिशों ने प्रति आक्रमण किया और लक्ष्मीबाई बुरी तरह से जख्मी हो गई। चूंकि वे नहीं चाहती कि ब्रिटिश उनके शरीर पर कब्जा करें अतः उन्होंने एक सन्यासी को उन्हें दफनाने के लिए कहा। 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु पर उनके शरीर को उनकी इच्छा के अनुसार दफन कर दिया गया। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के तीन दिन बाद ब्रिटिशों ने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया।
सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course
बिहार में विद्रोह के मुख्य संगठक 80 वर्ष के वृद्ध कुंवर सिंह थे, जो आरा के निकट जगदीशपुर के एक विध्वस्त और असंतुष्ट जमींदार थे। वे संभवतः इस विद्रोह के सबसे असाधारण सैन्य नेता और रणनीतिकार थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोह के एक अन्य असाधारण नेता थे। वे मद्रास के रहने वाले थे जहां उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के उपदेश देना शुरू किया था। जनवरी 1857 में वे उत्तर की ओर फैजाबाद आ गए जहाँ उन्होंने ब्रिटिश सेना की एक कंपनी के विरुद्ध बडे़ पैमाने पर युद्ध किया, जो उन्हें राजद्रोह के उपदेश से रोकने के लिए भेजी गई थी। मई में जब आम विद्रोह भड़क उठा, तो वे अवध में इसके एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
हालांकि विद्रोह के महानतम नायक वे सिपाही थे जिनमें से कइयों ने युद्धभूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया और जिनमें से हजारों ने निस्वार्थ भावना से अपने जीवन का बलिदान दिया। अन्य किसी भी बात से भी अधिक यह उनका दृढ़ संकल्प और बलिदान ही था जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत से लगभग निष्कासित होने की कगार पर आ गया था। देशभक्ति के इस संघर्ष में यहां तक कि उन्होंने अपने गहरे धार्मिक मतभेदों का भी बलिदान कर दिया।
A.5 अनेकों बगावतें, ग़दर व विद्रोह
A.6 विद्रोह की कमज़ोरियाँ और निर्णायक अंत
 1857 का विद्रोह देश के व्यापक प्रदेश में व्याप्त था और यह काफी लोकप्रिय भी था। हालांकि यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी समुदायों और वर्गों को अपने आगोश में नहीं ले पाया। दक्षिण भारत और अधिकांश पश्चिमी और पूर्वी भारत अपेक्षाकृत शांत रहा। अनेक भारतीय राज्यों के शासकों और बडे़ जमींदारों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सक्रिय रूप से सहायता की। वास्तव में, भारत के केवल एक प्रतिशत प्रधान ही इस विद्रोह में शामिल हुए गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी कि ‘‘ये शासक और प्रधान उस तूफान के लिए बांध साबित हुए जो अन्यथा हमें एक विशाल लहर में बहा ले जाता।‘‘ हालांकि मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब में प्रचलित भावना इस बात के अनुकूल थी कि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहे।
1857 का विद्रोह देश के व्यापक प्रदेश में व्याप्त था और यह काफी लोकप्रिय भी था। हालांकि यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी समुदायों और वर्गों को अपने आगोश में नहीं ले पाया। दक्षिण भारत और अधिकांश पश्चिमी और पूर्वी भारत अपेक्षाकृत शांत रहा। अनेक भारतीय राज्यों के शासकों और बडे़ जमींदारों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सक्रिय रूप से सहायता की। वास्तव में, भारत के केवल एक प्रतिशत प्रधान ही इस विद्रोह में शामिल हुए गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी कि ‘‘ये शासक और प्रधान उस तूफान के लिए बांध साबित हुए जो अन्यथा हमें एक विशाल लहर में बहा ले जाता।‘‘ हालांकि मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब में प्रचलित भावना इस बात के अनुकूल थी कि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहे।
अधिकांश संपत्तिशाली वर्ग या तो विद्रोहियों के प्रति उदासीन थे या उनके विरुद्ध सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण थे। यहां तक कि अवध अनेक तालुकदार (बडे जमींदार), जो विद्रोह में शामिल हुए थे, उन्होंने भी विद्रोह का साथ तब छोड़ दिया जब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी संपत्तियां उन्हें वापस कर दी जाएँगी। इसके कारण अवध के किसानों और सैनिकों के लिए दीर्घकालीन गुरिल्ला अभियान जारी रखना काफी कठिन हो गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
साहूकार, जो ग्रामीणों के आक्रमणों के मुख्य लक्ष्य थे, स्वाभाविक रूप से विद्रोह के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। धीरे-धीरे व्यापारी भी विमुख होते गए। विद्रोही युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए उनपर भारी कर अधिरोपित करने के लिए या सेना को भोजन प्रदान करने के लिए उनके खाद्यान्न भंडारों पर कब्जा करने के लिए मजबूर थे। आमतौर पर व्यापारी अपनी संपत्ति और वस्तुओं को छिपा कर रखते थे और वे विद्रोहियों को मुत आपूर्ति प्रदान करने से इंकार कर देते थे। बंगाल के जमींदार, जो ब्रिटिशों द्वारा ही निर्माण किये गए थे, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। साथ ही बिहार के किसानों की उनके जमींदारों शत्रुता ने भी बंगाल के जमींदारों को भयभीत कर दिया था। उसी प्रकार, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बडे़ व्यापारियों ने भी ब्रिटिशों का इसलिए किया क्योंकि उन्हें मुख्य लाभ विदेशी व्यापार और ब्रिटिश व्यापारियों के साथ अच्छे संबंधों के कारण ही प्राप्त होता था।
- [col]
- आधुनिक शिक्षित भारतीय विद्रोहियों से उनके अंधविश्वासों के प्रति आग्रहों और प्रगतिशील सामाजिक उपायों के प्रति उनके विरोध के कारण उनसे घृणा करते थे। शिक्षित भारतीय अपने देश से पिछडे़पन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी यह गलत धारणा थी कि ब्रिटिश शासन उन्हें आधुनिकीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सामंतों और अन्य सामंती तत्वों के नेतृत्व में विद्रोही देश को पिछडेपन की ओर ले जायेंगे। उन्हें यह समझने के लिए आगे काफी दशक लगे कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में असमर्थ था, इसके विपरीत वह देश को और अधिक गरीबी में धकेल देगा और उसे पिछड़ा ही रखेगा। इस संबंध में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदृष्टा साबित हुए और उनके पास विदेशी शासन की बुराइयों, और उसे हटाने की आवश्यकता की बेहतर स्वाभाविक समझ थी। हालांकि शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग के विपरीत वे इस बात को नहीं समझ सके कि देश विदेशी शासन का शिकार इसीलिए हुआ था क्योंकि वह अभी तक सडी गली और अप्रचलित प्रथाओं, परंपराओं और संस्थाओं से चिपका हुआ था।
- वे यह देखने में असफल रहे कि राष्ट्रीय निर्वाण वापस सामंतवादी साम्राज्य की ओर जाने से नहीं प्राप्त होगा बल्कि यह आधुनिक समाज, वैज्ञानिक शिक्षा और आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की दिशा में आगे बढने से ही प्राप्त हो पायेगा। किसी भी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षित भारतीय राष्ट्र विरोधी या विदेशी शासन के प्रति वफादार थे। जैसे 1858 के बाद की घटनाओं ने दिखाया, वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। भारतीयों के बीच एकता का अभाव भारतीय इतिहास के इस कालखण्ड के दौरान अपरिहार्य था। आधुनिक राष्ट्रवाद अभी भी भारत में अज्ञात था। देशभक्ति का अर्थ था अपने छोटे से मोहल्ले, या क्षेत्र या अधिक से अधिक अपने राज्य के प्रति प्रेम। अखिल भारतीय हित और इस बात के प्रति जागरूकता, कि ये हित ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखते हैं, अभी भी हमारे यहां आना बाकी थी। वास्तव में 1857 के विद्रोह ने सभी भारतीय लोगों को साथ लाने में और उनमें यह जागरूकता जगाने में कि वे सभी एक ही देश के निवासी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- अंत में, एक बढ़ती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद, और विश्व भर में उसकी शक्ति की ऊँचाई, और अधिकांश भारतीय राजाओं और सामंतों द्वारा किया गया उसका समर्थन, सैन्य दृष्टि से विद्रोहियों के लिए काफी मजबूत और अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने देश में मनुष्यों, धन और शस्त्रों की असंख्य आपूर्ति की, हालांकि बाद में भारतीयों को अपने स्वयं के दमन की संपूर्ण कीमत चुकानी पड़ी।
इतिहास ने हमें बार-बार यह दिखाया है कि एक शक्तिशाली कृत संकल्प शत्रु के विरुद्ध युद्ध केवल साहस के बूते पर ही नहीं जीता जा सकता, जिसने अपने प्रत्येक कदम की व्यवस्थित योजना बनाई हुई है। विद्रोहियों को प्रारंभिक आघात तब लगा जब 20 सितंबर 1857 को एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा किया। वृद्ध सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। शाही राजकुमारों को बंदी बनाकर वहीं निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। सम्राट पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निष्कासित कर गया जहां 1862 में अपनी उस दुर्दशा पर विलाप करते हुए, जिसने उसे उसके जन्मस्थान के शहर से बहुत दूर दफन किया था, उनकी मृत्यु हुई। इसी के साथ मुगलों के उस महान घराने का अंत हुआ जिसकी अधिकांश महानता औरंगजेब के बाद ही नष्ट हो गई थी।
दिल्ली के पतन के साथ ही विद्रोह का केंद्रबिंदु ही नष्ट हो गया। विद्रोह के अन्य नेताओं ने वीरतापूर्ण परंतु असमान संघर्ष जारी रखा, जिसमें ब्रिटिशों ने उनके विरुद्ध शक्तिशाली आक्रमण किये। जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हेवलॉक, नील कैंपबेल और ह्यूग रोज कुछ ऐसे ब्रिटिश सेनापति थे जिन्हें इस अभियान के दौरान सैन्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक के बाद एक इस विद्रोह के सभी महान नेताओं का पतन हुआ।
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिशों का अधिकार पूर्णतः पुनः प्रस्थापित हो गया, परंतु विद्रोह पूरी तरह बेकार नहीं गया। यह हमारे इतिहास का श्रेष्ठ मील का पत्थर है। हालांकि यह पुराने तरीकों से और पारंपरिक नेतृत्व के अधीन भारत को बचाने का एक अतिसाहसिक प्रयास था, फिर भी यह भारतीय लोगों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला संघर्ष था। इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
1857 के ओजस्वी और देशभक्तिपूर्ण संघर्ष, और इसके पहले की विद्रोहों की श्रृंखला ने भारत के लोगों के दिलोदिमाग पर एक अविस्मरणीय छाप छोडी है, इसने ब्रिटिश शासन के विरोध की बहुमूल्य स्थानीय परंपराओं की स्थापना की है, और बाद के स्वतंत्रता के संघर्ष में एक सर्वकालिक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। इस विद्रोह के नायक शीघ्र ही देश भर में पारिवारिक नाम बन गए, हालांकि उनके नामों के उच्चारण मात्र से शासकों की त्योरियां चढ़ जाती थीं।
A.7 19वीं और 20वीं सदी के अन्य आंदोलन
आदिवासी आंदोलन
जातीय आन्दोलन व किसान आन्दोलन
A.9 उन दिनों का भारत
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]
[next]
Lecture continues here ...
B. १८५७ पश्चात का भारत
B.1 प्रस्तावना
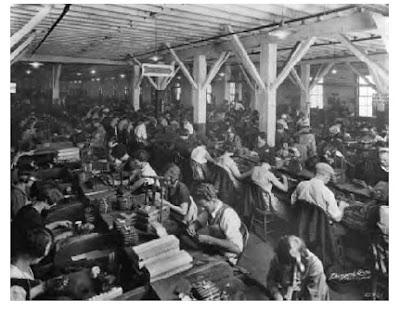 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक ज़ोरदार झटका दिया और इसके पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। भारत की संरचना और नीतियों में, विद्रोह के बाद के दशकों में सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार के परिवर्तन में अधिक महत्वपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद के एक नये चरण का उद्घाटन था।
1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक ज़ोरदार झटका दिया और इसके पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। भारत की संरचना और नीतियों में, विद्रोह के बाद के दशकों में सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार के परिवर्तन में अधिक महत्वपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद के एक नये चरण का उद्घाटन था।
19वीं सदी के उत्तरार्ध ने औद्योगिक क्रांति के गहन प्रसार को देखा। धीरे-धीरे यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे अन्य देशों का औद्योगीकरण होने लगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के निर्माण और वित्तीय सर्वोच्चता का अंत हो गया। पूंजी निवेश के लिए कच्चे माल और बाज़ार के लिए दुनिया भर में तीव्र प्रतिस्पर्धा अब शुरू हो गई। ताजा औपनिवेशिक वर्चस्व के लिये खुले क्षेत्र दुर्लभ हो गये। अतः काॅलोनियों और अर्ध-काॅलोनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़कर और कड़ी हो गयी। नए देशों से विश्व पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति के लिए एक चुनौती से सामना होने के कारण, ब्रिटेन ने अपने मौजूदा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक ज़ोरदार प्रयास शुरू किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
इसके अलावा, 1850 के बाद ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी राशि भारत सरकार के रेल्वे व ऋणों में निवेषित थी, व कुछ राषि चाय बागानों, कोयला खनन, जूट मिलों, जहाजरानी, व्यापार, व बैंकिंग में निवेश की गई थी। आर्थिक और राजनीतिक खतरों से इस ब्रिटिश पूंजी को सुरक्षित रखना अब ज़रूरी हो गया था। भारत में ब्रिटिश शासन और भी अधिक मजबूती से संभालना आवश्यक था। नतीजतन शाही नियंत्रण और साम्राज्यवादी विचारधारा की एक नए सिरे से शुरूआत हुई जो इन राजप्रतिनिधियों जैसे लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन और सब से अधिक कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीतियों में परिलक्षित हुआ। (Lytton, Dufferin, Lansdowne, Elgin, Curzon)
B.2 अंग्रेज़ प्रशासन में वैधानिक परिवर्तन
 1858 में संसद के एक अधिनियम ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी। भारत पर अधिकार पहले कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निदेशकों द्वारा किया जाता था, वहीं अब यह शक्ति भारत के लिए एक परिषद द्वारा समर्थित एक ‘राज्य के सचिव’ द्वारा प्रयोग की जाने वाली थी। राज्य के सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंड़ल के सदस्य थे और इस तरह वे संसद के प्रति जिम्मेदार थे। इस प्रकार भारत में परम शक्ति ब्रिटिश संसद के साथ बनी रही।
1858 में संसद के एक अधिनियम ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी। भारत पर अधिकार पहले कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निदेशकों द्वारा किया जाता था, वहीं अब यह शक्ति भारत के लिए एक परिषद द्वारा समर्थित एक ‘राज्य के सचिव’ द्वारा प्रयोग की जाने वाली थी। राज्य के सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंड़ल के सदस्य थे और इस तरह वे संसद के प्रति जिम्मेदार थे। इस प्रकार भारत में परम शक्ति ब्रिटिश संसद के साथ बनी रही।
इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा पहले की ही तरह गवर्नर जनरल (जिसे वायसराॅय या सरकार के निजी प्रतिनिधि का खिताब दिया गया था) के द्वारा चलाई जाती थी। समय बीतने के साथ वायसराॅय की स्थिति नीति-निर्माण एवं निष्पादन के मामले में ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में कम होती गई। राज्य के सचिव ने प्रशासन के सूक्ष्मतम विवरण को नियंत्रित किया। इस प्रकार भारतीय मामलों पर अंतिम और विस्तृत नियंत्रण और दिशा, लंदन (भारत से हजारों मील दूर) से आया करती थी। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, भारतीय राय का प्रभाव पहले की तुलना में सरकार की नीति पर और भी कम पड़ा। दूसरी ओर, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों के भारत सरकार पर प्रभाव में वृद्धि हुई। भारतीय प्रशासन 1858 से पहले की तुलना में और अधिक प्रतिक्रियावादी (reactionary) बन गया व उदारवाद (liberalism) का ढ़ोंग भी अब धीरे-धीरे छोड़ दिया गया।
1858 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गर्वनर जनरल को एक कार्यकारी परिषद प्रदान की जिसके सदस्य विभागों के प्रमुख थे व गर्वनर-जनरल के सलाहकार भी थे। परिषद अनेक मुद्दे मताधिकार से तय करती थी किंतु इन्हें गवर्नर जनरल खारिज़ भी कर सकते थे।
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की भारतीय परिषद का विस्तार किया। यह अब विधि-निर्माण हेतु इंपीरियल (शाही) विधान परिषद के रूप में जानी जाती थी। गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारी परिषद मे छह से बारह गैर-अधिकारी सदस्यों को जोड़ने की शक्ति दी गई थी जिनमें से कम से कम आधे भारतीय या अंग्रेज़ हो सकते थे। इंपीरियल विधान परिषद के पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं थी और इसे प्राथमिक या कमजोर संसद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह महज एक सलाहकार निकाय था। यह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी महत्वपूर्ण उपायों (और किसी भी वित्तीय उपायों) पर चर्चा नहीं कर सकता था। इसका बजट पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। यह प्रशासन की किसी कार्रवाई पर चर्चा नहीं कर सकता था और न ही सदस्यों को भी उनके बारे में सवाल पूछ सकता था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
दूसरे शब्दों में, विधान परिषद का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा विधान परिषद द्वारा अनुमोदित कोई बिल तब तक एक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक उसे गवर्नर जनरल द्वारा पारित नहीं किया जाता। इस सब के शीर्ष पर, राज्य के सचिव इसके अधिनियमों को किसी भी रूप से अस्वीकार कर सकते थे। इस प्रकार, विधान परिषद का महत्वपूर्ण कार्य सरकारी उपायों को उसी हाल में और विधायी निकाय द्वारा पारित किया गया होने का स्वरूप देने के लिए गया था। सिद्धांत रूप में, गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों को भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद से जोड़ा गया था। लेकिन विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की संख्या में कम थी और वे भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं थे। वे हमेशा प्रधानों, उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों, या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों मे से गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते थे। वे भारतीय लोगों की या बढ़ती राष्ट्रवादी राय के प्रतिनिधि नहीं थे। भारत सरकार 1858 के पहले जैसी एक विदेशी तानाशाह के रूप में बनी रही। यह कोई दुर्घटना नहीं थी अपितु एक जागरूक नीति थी। चार्ल्स वुड, भारत के राज्य सचिव ने 1861 के भारतीय परिषद विधेयक को पेश करते हुए कहा था कि "हमारा अनुभव हमें सिखाता है कि जब एक प्रभावशाली जाति दूसरों पर राज करती है, तो तानाशही उसका सबसे न्यूनतम शोषक प्रकार है।"
B.3 प्रांतीय प्रशासन
ब्रिटिश राज ने भारत को प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रांतों में विभाजित किया था, जिनमें से तीन - बंगाल, मद्रास व बम्बई की प्रेसीडेंसी के रूप में जाने जाते थे। प्रेसीडेंसी क्राउन द्वारा नियुक्त किये गये एक गवर्नर और उसकी तीन की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी। प्रेसीडेंसी सरकारों के पास अन्य प्रांतीय सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां होती थी जो लेफ्टिनेंट गर्वनर व चीफ कमिश्नरों (आयुक्त) द्वारा प्रशासित होते थे।
1833 से पहले प्रांतीय सरकारों ने स्वायत्तता का आनंद लिया था पर कानून पारित करने की इनकी शक्ति छीन ली गयी थी जब और अब इनके खर्च पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण था। लेकिन जल्द ही यह अनुभव हुआ कि भारत जैसे विशाल देश को सख्त केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर कुशलता से प्रशासित नहीं किया जा सकता।
 चरम केंद्रीयकरण की बुराई वित्त के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट थी। देश भर में विभिन्न स्रोतों से राजस्व केंद्र पर एकत्र हुआ करते और उसके बाद प्रांतीय सरकारों के द्वारा वितरित किए जाते। केन्द्र सरकार ने प्रांतीय व्यय की छोटी से छोटी जानकारी पर सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में काफी खर्चीली साबित हुई। केन्द्र सरकार का एक प्रांतीय सरकार पर राजस्व के कुशल संग्रह पर निगरानी रखना या उसके व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अधिकारियों ने इसलिए सार्वजनिक वित्त विकेंद्रीकृत करने का फैसला किया।
चरम केंद्रीयकरण की बुराई वित्त के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट थी। देश भर में विभिन्न स्रोतों से राजस्व केंद्र पर एकत्र हुआ करते और उसके बाद प्रांतीय सरकारों के द्वारा वितरित किए जाते। केन्द्र सरकार ने प्रांतीय व्यय की छोटी से छोटी जानकारी पर सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में काफी खर्चीली साबित हुई। केन्द्र सरकार का एक प्रांतीय सरकार पर राजस्व के कुशल संग्रह पर निगरानी रखना या उसके व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अधिकारियों ने इसलिए सार्वजनिक वित्त विकेंद्रीकृत करने का फैसला किया।
केंद्रीय और प्रांतीय वित्त अलग करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में लिया गया था। प्रांतीय सरकार को पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, और सड़क जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए केंद्रीय राजस्व की निश्चित रकम दी गई और उन्हे अपनी इच्छा से उनके प्रशासन के लिए कहा गया। लॉर्ड मेयो की इस विकेंद्रीकृत नीति को लाॅर्ड लिटन द्वारा 1877 में भूमि राजस्व, आबकारी, सामान्य प्रशासन, और कानून एवं न्याय जैसे कुछ अन्य मदों में विस्तारित किया गया। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए एक प्रांतीय सरकार को, आबकारी करों, और आयकर जैसे कुछ स्रोतों से उस प्रांत से प्राप्त आय का एक निश्चित हिस्सा मिलता था। इन व्यवस्थाओं में आगे परिवर्तन 1882 में हुआ। प्रांतों के लिए निर्धारित अनुदान देना समाप्त हो गया और एक प्रांत को निश्चित स्रोतों और अन्य स्रोतों से आय का एक निश्चित हिस्सा या संपूर्ण आय दिया जाने लगा। इस प्रकार, राजस्व के सभी स्रोतों को अब तीन - सामान्य, प्रांतीय और केन्द्र-प्रांतों के बीच में बंटने वाला - भागों में बांट दिया गया।
वित्तीय विकेंद्रीकरण के विभिन्न उपायों का मतलब यह नहीं था कि वास्तव में असली प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय प्रशासन में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। इन प्रशासनिक पुनर्गठनों का मुख्य उद्देश्य खर्च कम रखने के लिए और आय को बढ़ाना ही था। सिद्धांत और अभ्यास दोनों रूपों में, केंद्रीय सरकार सर्वोच्च बनी रही और प्रांतीय सरकारों पर अधिक प्रभाव और विस्तृत नियंत्रण जारी रहा। यह अपरिहार्य था, और केंद्रीय व प्रांतीय सरकारें पूरी तरह से राज्य और ब्रिटिश सरकार के सचिव के अधीन थीं। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course
B.4 स्थानीय निकाय (Local bodies)
 वित्तीय कठिनाइयों ने नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड़ों (मंड़लों) के माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देकर प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए सरकार को मज़बूर किया। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने धीरे-धीरे यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। यूरोप में साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण के नए तरीकों के जन्म लेने के साथ भारत के साथ बढ़ते संपर्क ने अर्थव्यवस्था, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोपीयों के कुछ तरीकों को भारत में प्रत्यारोपित किये जाने को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा, बढ़ते भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागरिक जीवन में सुधार की शुरूआत की मांग की। इस प्रकार जनता ने स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कें, और अन्य नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत को तेज़ी से महसूस किया। सरकार अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर भारी खर्च के कारण वित्त में विकार पहले से मौजूद थे। मौजूदा कराधान का बोझ पहले से ही गरीबों पर बहुत भारी था। इसे और बढ़ाने पर सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होने की संभावना थी। नए करों के माध्यम से आय में वृद्धि नहीं हो सकी। दूसरी ओर सरकार विशेष रूप से उच्च वर्गों, ब्रिटिश सिविल सेवकों, बागान मालिकों और व्यापारियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी। अधिकारियों ने महसूस किया लोगों को नए करों के भुगतान पर दुख नहीं होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके पैसे को उनके स्वयं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इसलिए स्थानीय निकायों को स्थानीय करों के माध्यम से प्राप्त वित्त को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी स्थानीय सेवाओं के लिए हस्तांतरित करने का फैसला किया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों के गठन के लिए एक और कारण से दबाव बनाया था। प्रशासन के साथ कुछ भारतीयों को जोड़ कर उनके राजनीतिक रूप से असन्तुष्ट होने को रोका जा सकता था। यह सहयोग भारत में ब्रिटिश शक्ति के एकाधिकार को खतरे में ड़ाले बिना स्थानीय निकायों के स्तर पर हो सकता था।
वित्तीय कठिनाइयों ने नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड़ों (मंड़लों) के माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देकर प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए सरकार को मज़बूर किया। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने धीरे-धीरे यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। यूरोप में साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण के नए तरीकों के जन्म लेने के साथ भारत के साथ बढ़ते संपर्क ने अर्थव्यवस्था, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोपीयों के कुछ तरीकों को भारत में प्रत्यारोपित किये जाने को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा, बढ़ते भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागरिक जीवन में सुधार की शुरूआत की मांग की। इस प्रकार जनता ने स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कें, और अन्य नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत को तेज़ी से महसूस किया। सरकार अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर भारी खर्च के कारण वित्त में विकार पहले से मौजूद थे। मौजूदा कराधान का बोझ पहले से ही गरीबों पर बहुत भारी था। इसे और बढ़ाने पर सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होने की संभावना थी। नए करों के माध्यम से आय में वृद्धि नहीं हो सकी। दूसरी ओर सरकार विशेष रूप से उच्च वर्गों, ब्रिटिश सिविल सेवकों, बागान मालिकों और व्यापारियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी। अधिकारियों ने महसूस किया लोगों को नए करों के भुगतान पर दुख नहीं होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके पैसे को उनके स्वयं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इसलिए स्थानीय निकायों को स्थानीय करों के माध्यम से प्राप्त वित्त को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी स्थानीय सेवाओं के लिए हस्तांतरित करने का फैसला किया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों के गठन के लिए एक और कारण से दबाव बनाया था। प्रशासन के साथ कुछ भारतीयों को जोड़ कर उनके राजनीतिक रूप से असन्तुष्ट होने को रोका जा सकता था। यह सहयोग भारत में ब्रिटिश शक्ति के एकाधिकार को खतरे में ड़ाले बिना स्थानीय निकायों के स्तर पर हो सकता था।- [col]
- स्थानीय निकायों का पहली बार 1864 और 1868 के बीच गठन किया गया, लेकिन लगभग हर मामले में उनमें नामजद (दवउपदंजमक) सदस्य शामिल थे और वे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में चलते थे। इसलिए स्थानीय निकायों ने स्वयं-सरकार का स्वरूप कभी नहीं लिया व न ही बुद्धिमान भारतीयों ने इसे ऐसे स्वीकार किया। उन्होंने इसे लोगों से अतिरिक्त करों की निकासी के साधन के रूप में देखा। एक बहुत संकोची कदम, लार्ड रिपन की सरकार द्वारा 1882 में लिया गया था।
- एक सरकारी संकल्प ने नीति निर्धारित की कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रशासन होगा, जो गैर-अधिकारी सदस्यों के माध्यम से होगा। इन गैर-अधिकारी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा जब अधिकारियों को आवश्यकता महसूस होगी तब किया जाएगा। प्रस्ताव ने स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी अधिकारी के चुनाव की अनुमति दी।
- लेकिन निर्वाचित सदस्य सभी जिला बोर्डों में और नगर पालिकाओं में अल्पमत थे, इसके अलावा चूँकि मतदान का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था अतः उनका चुनाव बहुत कम वोटरों द्वारा किया गया था। गैर-अधिकारी धीरे-धीरे नगर निगम समितियों के अध्यक्ष बन गये, हालांकि जिला अधिकारियों ने जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखा। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
सरकार ने स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करने के लिए और अपने स्वयं के विवेक पर उन्हें निलंबित करने का अधिकार अपने पास रखा। परिणामस्वरूप कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी शहरों को छोड़कर, स्थानीय निकायों ने सिर्फ सरकार के विभागों की तरह कार्य किया और स्थानीय स्वयं-सरकार के ये अच्छे उदाहरण नहीं थे। राजनैतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और कालांतर में वे स्थानीय स्वयं सरकार के प्रभावी अंगों में तब्दील किया जा सकते हैं इस उम्मीद में इन स्थानीय निकायों में सक्रिय रूप से काम किया।
B.5 सेना में परिवर्तन
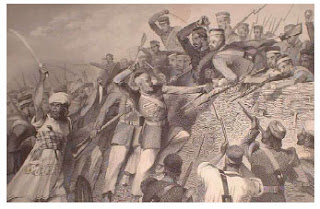 1858 के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया, क्योंकि सरकार को एक और ‘विद्रोह’ की पुनरावृत्ति रोकनी थी। शासक समझ रहे थे कि उनकी बंदूकें ही उनके राज की ठोस बुनियाद थीं। कई कदम भारतीय सैनिकों की विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए उठाए गये। सबसे पहले, सेना का वर्चस्व यूरोपीय शाखा द्वारा हो, यह आश्वस्त किया गया। सेना में भारतीयों का गोरों से अनुपात बंगाल सेना में एक से दो और मद्रास और बंबई सेनाओं में दो से पाँच पर तय किया गया था। इसके अलावा, यूरोपीय सैनिकों को महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों व पदों पर रखा गया था। महत्वपूर्ण तोपखाने और बाद में (20वीं सदी में) टैंकों और बख्तरबंद कोर यूरोपीय हाथ में विशेष रूप से रखे गए थे। अधिकारी कोर (बवतचे) से भारतीयों को अलग रखने की पुरानी नीति को सख्ती से बनाए रखा गया था। 1914 तक कोई भी भारतीय एक सूबेदार के पद से अधिक नहीं बढ़ सका था।
1858 के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया, क्योंकि सरकार को एक और ‘विद्रोह’ की पुनरावृत्ति रोकनी थी। शासक समझ रहे थे कि उनकी बंदूकें ही उनके राज की ठोस बुनियाद थीं। कई कदम भारतीय सैनिकों की विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए उठाए गये। सबसे पहले, सेना का वर्चस्व यूरोपीय शाखा द्वारा हो, यह आश्वस्त किया गया। सेना में भारतीयों का गोरों से अनुपात बंगाल सेना में एक से दो और मद्रास और बंबई सेनाओं में दो से पाँच पर तय किया गया था। इसके अलावा, यूरोपीय सैनिकों को महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों व पदों पर रखा गया था। महत्वपूर्ण तोपखाने और बाद में (20वीं सदी में) टैंकों और बख्तरबंद कोर यूरोपीय हाथ में विशेष रूप से रखे गए थे। अधिकारी कोर (बवतचे) से भारतीयों को अलग रखने की पुरानी नीति को सख्ती से बनाए रखा गया था। 1914 तक कोई भी भारतीय एक सूबेदार के पद से अधिक नहीं बढ़ सका था।एक ब्रिटिश-विरोधी विद्रोह में पुनः भारतीय सैनिक एकजुट ना हो जायें, अतः सेना के भारतीय खंड का निर्धारण ‘संतुलन और समबल’ या ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति से किया गया था।
- [message]
- जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव की कोशिश सेना की भर्ती में की जाती थी।
- भारतीयों के ‘सामरिक’ (martial) और ‘गैर-सामरिक’ (non-martial) वर्गों में बंटे होने की एक मिथ्या बनाई गई।
- अवध, बिहार, मध्य भारत, और दक्षिण भारत के सैनिकों जिन्होंने पहली बार भारत की जीत में ब्रिटिश मदद की थी लेकिन बाद में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था उन्हें ‘गैर-सामरिक’ घोषित किया गया। उन्हें अब एक बड़े पैमाने पर सेना में नहीं लिया गया।
- दूसरी ओर पंजाबी, गुरखा, और पठान जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता प्रदान की थी उन्हें सामरिक घोषित किया गया और बड़ी संख्या में भर्ती की गई।
- 1875 तक ब्रिटिश भारतीय सेना के आधे सैनिक पंजाब से भर्ती किये गये थे। इसके अलावा, भारतीय रेजिमेंटों को विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण बना दिया ताकि वे संतुलन बनाएं रखें।
- यह जाति-आधारित कार्य सैनिकों के बीच प्रोत्साहित किया गया जिससे उनमें सांप्रदायिक, जाति, आदिवासी और क्षेत्रीय वफादारी की भावना विकसित हो न कि राष्ट्रवाद की। उदाहरण के लिए जाति और सांप्रदायिक कंपनियां सभी रेजिमेंटों में शुरू किए गए।
चार्ल्स वुड, भारत के लिए राज्य सचिव, ने 1861 में वायसराय कैनिंग को लिखाः
 ‘‘मैं फिर से एक महान सेना नहीं देखना चाहता जिसे अपनी शक्ति में वैसा ही विश्वास हो कि वो एक साथ विद्रोह हेतु उठ खड़ी हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो अगली रेजिमेंट को इतना मतभिन्न होना चाहिए कि वह इसे मारने के लिए तैयार हो’’।
‘‘मैं फिर से एक महान सेना नहीं देखना चाहता जिसे अपनी शक्ति में वैसा ही विश्वास हो कि वो एक साथ विद्रोह हेतु उठ खड़ी हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो अगली रेजिमेंट को इतना मतभिन्न होना चाहिए कि वह इसे मारने के लिए तैयार हो’’।
इस प्रकार भारतीय सेना एक विशुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही। इसके अलावा हर प्रयास किया गया वे बाकी की जनसंख्या के जीवन और विचारों से अलग रहें। उन्हे हर-संभव तरह से राष्ट्रवादी विचारों से अलग रखा गया था। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक पहुँचने से रोका गया। बाद में यह नीति भारतीय सेना को लंबे समय तक और वर्गों में बांटने में विफल रही। ऐसे सभी प्रयासों ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
[##leaf## आधुनिक भारतीय रक्षा, सशस्त्र बल और अर्ध-सैनिक बलों के बारे में पढ़ें]
[##leaf## आधुनिक भारतीय रक्षा, सशस्त्र बल और अर्ध-सैनिक बलों के बारे में पढ़ें]
भारतीय सेना वक्त के साथ में एक बहुत महंगी सैन्य मशीन बन गयी। 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52 प्रतिशत इसमें अवशोषित हुआ। इसका कारण सिर्फ एक नहीं था। भारत उस समय का सबसे बेशकीमती औपनिवेशिक कब्जा था। इसे लगातार रूस, फ्रांस और जर्मनी के साम्राज्यवाद की होड़ से बचाना था। इसलिए भारतीय सेना के आकार में एक बड़ी वृद्धि हुई। दूसरा, भारतीय सैनिकों को अकेले भारत की रक्षा के लिए नहीं बनाए रखा गया था। भारतीय सेना ब्रिटिश सत्ता का एशिया और अफ्रीका में संपत्ति के विस्तार और समेकन के लिए मुख्य साधन थी। अंततः, सेना के ब्रिटिश अनुभाग द्वारा भारत पर कब्जे रखने के रूप में यह देश भर में ब्रिटिश पकड़ की अंतिम गारंटी थी। इसकी लागत भारतीय राजस्व से निकलती थी और यह वास्तव में उन पर एक बहुत भारी बोझ था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
B.6 सार्वजनिक सेवाएं (Public Services)
अभी तक हमने देखा कैसे सरकार चलाने में भारतीयों का नियंत्रण नाममात्र था। कानून-व्यवस्था के नियमों को बनाने या निर्धारित करने की अनुमति भारतीयों को नहीं थी। यही नहीं, भारतीयों को नीतियाँ बनाने वाली नौकरशाही में भी कोई जगह नहीं मिली। जिन प्रशासनिक पदों में शक्ति और जिम्मेदारी होती थी उन सारे पदों पर भारतीय जन सेवा (भारतीय सिविल सर्विसेज) के सदस्य विराजमान थे। इनकी नियुक्ति लंदन में एक खुली वार्षिक परीक्षा के द्वारा होती थी। एक आम भारतीय इस वार्षिक परीक्षा में बैठ सकता था। रबिन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जब 1863 में उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। हर साल एक-दो भारतीय इस बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल कर तो लेते थे परन्तु अंग्रेज़ों के मुकाबले भारतीयों की संख्या काफी कम रहती थी। व्यवहार में यह परीक्षा भारतीयों के लिए बड़ी ही मुश्किल थी। इसके कई कारण थे जैसे इस परीक्षा का लंदन में होना और परीक्षा का अंग्रेजी भाषा माध्यम। इतना ही नहीं, यह परीक्षा लैटिन और यूनानी पाठों पर आधारित थी जिसे समझने के लिए विदेश में लम्बी और महँगी पढ़ाई करनी होती थी। 1878 में इस परीक्षा में बैठने की उम्र को 23 से घटा कर 19 वर्ष कर दिया गया। जब यह 23 साल के भारतीय परीक्षार्थियों के लिए मुश्किल थी, तो 19 साल के छात्रों के लिए असंभव-सी थी।
प्रशासन के अन्य विभागों में जैसे पुलिस, डाक, जनकार्य, दवाइयां, प्रौद्योगिकी और बाद में रेलवे, उच्च और अधिक आय वाले पद अंग्रेजो के लिए आरक्षित थे।
अंग्रेजी सरकार का ऐसा सामरिक व्यवहार आकस्मिक नहीं था। देश के शासकों को यह विश्वास था की अंग्रेजी बादशाहत को कायम रखने के लिए यह कदम जरुरी है। लार्ड किम्बर्ले (राज्य के सचिव) ने 1893 में यह बात कही “यह अपरिहार्य है कि भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय पर्याप्त संख्या में रहें”। वाइसराॅय लार्ड लैंसडाॅन ने जोर दिया “इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरुरी है की यह यूरोपीय हाथों में रहे”।
1918 तक भारतीय दबाव में विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण सम्भव हो सका। किंतु देश पर नियंत्रण और अधिकार रखने वाले पदों पर अभी भी अंग्रेजों का ही दबदबा था। लोगों ने जल्द ही यह समझ लिया कि प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण के बावजूद राजनैतिक तौर पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था। जो भारतीय इन पदों पर नियुक्त किये गए थे वह उनके नुमांइदे थे जो भक्तिपूर्वक अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों को पूरा कर रहे थे।
B.7 भारतीय रियासतों से सम्बन्ध
 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति बदली। तब तक अंग्रेज़ भारत की विभिन्न रियासतों को हथियाने के हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहते। यह नीति 1857 में स्थगित कर दी गई। भारत के अधिकतर राज्यों ने न सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ दिया बल्कि बाद में इस विद्रोह को दबाने में उनकी भरपूर मदद भी की। लार्ड कैनिंग जो उस समय के वाइसराय थे, उनके शब्दों में “इन्होंने तूफान में रुकावट का काम किया”। इसके मद्देनज़र अंग्रेज़ी सरकार ने इन राज्यों को न सिर्फ अपनी विरासत कायम रखने का भरोसा दिया बल्कि भविष्य में इन्हें विलय से अलग रखने का भी वादा किया। अंग्रेज़ सरकार ने यह भी सीख ली की भविष्य में यह छोटे रियासती राज्य किसी भी तरह के विद्रोह से निपटने में उनके मददगार साबित हो सकते हैं। 1860 में लार्ड कैनिंग ने लिखाः
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति बदली। तब तक अंग्रेज़ भारत की विभिन्न रियासतों को हथियाने के हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहते। यह नीति 1857 में स्थगित कर दी गई। भारत के अधिकतर राज्यों ने न सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ दिया बल्कि बाद में इस विद्रोह को दबाने में उनकी भरपूर मदद भी की। लार्ड कैनिंग जो उस समय के वाइसराय थे, उनके शब्दों में “इन्होंने तूफान में रुकावट का काम किया”। इसके मद्देनज़र अंग्रेज़ी सरकार ने इन राज्यों को न सिर्फ अपनी विरासत कायम रखने का भरोसा दिया बल्कि भविष्य में इन्हें विलय से अलग रखने का भी वादा किया। अंग्रेज़ सरकार ने यह भी सीख ली की भविष्य में यह छोटे रियासती राज्य किसी भी तरह के विद्रोह से निपटने में उनके मददगार साबित हो सकते हैं। 1860 में लार्ड कैनिंग ने लिखाः
‘‘सर जॉन मैल्कम ने बहुत पहले यह कहा था की पूरे भारत को जिला-वार बना दिया जाए, तो तय नहीं है कि हमारी हुकूमत 50 साल से ज्यादा चले, पर अगर हम कुछ भारतीय राज्यों को राजनीति से दूर रख शाही उपकरण की तरह इस्तेमाल करें तो हम इस देश में तब तक राज कर सकते हैं जब तक हम नौसेनिक शक्ति में इनसे ऊपर रहें। इस राय में दम पहले भी था और हाल के घटनाक्रम ने हमें इस विषय पर विशेष नज़र डालने के लिए मजबूर कर दिया है’’।
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
इस वजह से इन रियासती राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों की तरह जीवित रखने का फैसला किया गया। इस पर अंग्रेज इतिहासकार पी.ई. राॅबर्टस् ने लिखा “राज्यों को सुरक्षा बांध की तरह सहेज कर बनाए रखना अंग्रेज़ सरकार की पहले से बनी एक नीति है।’’
- [col]
- स्थायीकरण रियासतों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनायी हुई नीति का केवल एक पहलू था। इसके अलावा अंग्रेज़ों के लिए इन राज्यों की अधीनता भी एक प्रमुख उद्देश्य था। 1857 के विद्रोह से पहले भी अंग्रेजों ने इन राज्यों के अंदरूनी मसलों में दखलअंदाजी करते रहते थे। सैद्धान्तिक तौर पर यह राज्य उनके लिए सहायक किंतु संप्रभु शक्तियां थी।
- बदले में इन राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत को सर्वोपरि शक्ति के रूप में मानना पड़ा। 1876 में महारानी विक्टोरिया ने अंग्रेजी हुकूमत की बादशाहत को साबित करने के लिए अपने आप को ‘‘भारत की साम्राज्ञी’’ का खिताब दे दिया। लाॅर्ड कर्ज़न ने बाद में यह साफ कर दिया कि यह राज्य अंग्रेजी सल्तनत के एजेंट मात्र हैं।
- भारतीय राजाओं ने भी इसमें हामी भरी ताकि उनका राज्य उनके पास रहने दिया जाये।
सर्वोच्च शक्ति होने के नाते अंग्रेज़ सरकार ने इन छोटे राज्यों के अंदरूनी मसलों में भी निगरानी करने का अधिकार बनाए रखा। दखलंदाजी न सिर्फ दैनिक काम काज में होती थी, बल्कि अंग्रेज़ सरकार राज्यों के मंत्रियों को रखने और हटाने में भी अपनी राय रखने लगी। कभी-कभी वे शासको की ताकतों को मिटा या दबा देते थे। उनका एक मकसद ये भी था कि राज्यों को आधुनिक करें जिससे कि उसे अंग्रेज़ी हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सके। भारत में रेलवे, डाक, दूरसंचार, मुद्रा और आम आर्थिक जीवन शैली के विकास से उनके एकीक्रम और दखलअंदाजी को बढ़ावा मिल रहा था। अंग्रेज़ राजसी रियासतों में उठ रहे व्यापक लोकतांत्रिक व राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी सचेत हो चुके थे। वे राजाओं को इन्हें कुचलने में मदद करते किंतु राजाओं की गंभीर प्रशासनिक चूकों को भी ठीक करने का प्रयास करते। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
B.8 प्रशासनिक नीतियां
1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजी सरकार का भारतियों के प्रति रवैया और नीतियां दोनों ही बदतर हो गए। 1857 तक जहाँ उनके कदम रुक-रुक कर ही सही पर भारत के आधुनिकीकरण की तरफ उठे, इस विद्रोह के बाद वो कदम प्रतिक्रियावादी बन गए थे। इतिहासकार पर्सिविअल स्पीयर के शब्दों में “भारत सरकार का विकास के साथ हनीमून समाप्त हो गया था”।
अब तक यह स्पष्ट है की प्रशासनिक व्यवस्था के दो मुख्य अंग सेना और सिविल सेवा को भारतीयों से दूर कर, उनकी अपने ही देश को चलने में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया था। विद्रोह से पहले तक कम से कम बोल-चाल में अंग्रेज़ांे ने यह अफवाह फैला रखी थी की वह भारतीयों को शासन करने के प्रशिक्षण के बाद राजनितिक फैसले करने के योग्य बना कर देश उनके हाथो में दे देंगे परन्तु अब यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा था की भारतीय निहित सामाजिक और सांस्कृतिक दोष के कारण देश चलाने के योग्य नहीं हैं और अंग्रेज सरकार को ही भारत में अनिश्चित काल तक भारत देश में शासन करना होगा। यह प्रतिक्रियावादी निति विभिन्न क्षेत्रों में नजर आने लगी थी।
B.9 बाँट कर राज करने की नीति (Divide and Rule)
 अंग्रेज़ों ने भारत के राज्यों में एकता के अभाव का फायदा उठा कर और इन में फूट डाल कर कब्ज़ा किया था। 1870 के बाद उनकी यह नीति और विस्तृत हो गयी। उन्होंने राजाओं को लोगों के खिलाफ, प्रान्त को प्रान्त के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ और समूह को समूह के खिलाफ और सबसे डरावनी बात, हिन्दू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया।
अंग्रेज़ों ने भारत के राज्यों में एकता के अभाव का फायदा उठा कर और इन में फूट डाल कर कब्ज़ा किया था। 1870 के बाद उनकी यह नीति और विस्तृत हो गयी। उन्होंने राजाओं को लोगों के खिलाफ, प्रान्त को प्रान्त के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ और समूह को समूह के खिलाफ और सबसे डरावनी बात, हिन्दू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया।
1857 में हिन्दू-मुस्लिम एकता देख कर अंग्रेज़ काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को रोकने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को विखंड़ित करने की ठान ली थी। विद्रोह के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की ज़मीन कब्जे में ली और हिदुओं को अपना चहेता घोषित कर दिया। 1870 के बाद उन्होंने इस नीति में बदलाव किया और उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आन्दोलन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।
सरकारी नौकरियों के लोभ के जरिये अंग्रेजों ने धार्मिक मसलों पर पढ़े-लिखे भारतीयों में अलगाव बनाने की नीति अपनाई। औद्योगीकरण और करोबार के अभाव में पढ़े-लिखे भारतीयों के पास सरकारी नौकरी के सिवा और कोई रोजगार का अवसर नहीं था और इस तरह वह अंग्रेजों पर आश्रित हो चुके थे। भारतीयों के लिए चंद पद थे जिसको पाने के लिए प्रतियोगिता के भाव को अंग्रेजों ने नफरत, भेद भाव फैलाने में उपयोग किया। उन्होंने सरकारी नियुक्तियां करने में साम्प्रदायिका दर्षाते हुए हिंदुओं व मुस्लिमों को बांटने का पूरा कार्य किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
B.10 शिक्षित भारतीयों से भेद-भाव
1857 और उससे पहले अंग्रेजों ने भारत में उच्च पढ़ाई के लिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय बनवाए। काफी अंग्रेज़ अधिकारियों ने इस बात की सराहना की कि शिक्षित भारतीयों ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। परन्तु जैसे ही पढ़े-लिखे भारतीयों की तादाद बढ़ी, यह भारतीय अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों के भेद समझने और जानने लगे, जिसके बाद उन्होंने शासन में भारतीय हिस्सेदारी की मांग उठानी शुरू कर दी। पढ़ेे-लिखे भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों के तेवर और तीखे तब हो गए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके उपरांत अंग्रेजी सरकार ने उच्च शिक्षा को रोकना शुरू कर दिया और पढ़े-लिखे भारतीयों को ‘विद्रोही बाबू’ बुलाने लगे।
इस प्रकार अंग्रेज़ उन पढ़े-लिखे और पष्चिमी सभ्यता की समझ रखने वाले भारतीय समूह के बिलकुल खिलाफ हो गए। इन भारतियों के विकास की सोच अंग्रेजों के साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए एक खतरा थी। अपने इस कदम से अंग्रेज़ों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के विकास की कोई भी संभावना अब अंग्रेज़ों की कार्यषैली से तो उपजने वाली नहीं थी।
B.11 ज़मींदारों के प्रति रवैया
जहाँ अंग्रेज़ शिक्षित भारतीयों से अपनी दूरी बरकरार रखे हुए थे, वहीं अंग्रेज़ देश के ज़मींदारों और राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। हम यह पहले समझ चुके हैं किस तरह अंग्रेज़ों ने छोटे राज्यों और राजाओं को राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ बांध बना कर स्वहित में इस्तेमाल किया था। ज़मींदार भी राजाओं की ही तर्ज़ पर इस्तेमाल किये जा रहे थे। जैसे अवध के तालुकदारों और ज़मींदारों को उनकी ज़मीनें वापस कर दी गईं, व ज़मींदारों को ही उस प्रान्त का मुखिया समझा जाने लगा। उनके हितों और फायदे की रक्षा की जाने लगी। इन ज़मींदारों को उनकी ज़मीनों और किसानों के साथ आजादी से रहने दिया गया और इसी कारणवश यह ज़मींदारों का समूह राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ होने लगा। वाइसराय लार्ड लिटन ने 1876 में यह खुलेआम स्पष्ट कर दिया कि "अंग्रेज़ी हुकूमत की पहचान उन लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और सहानुभूति से है जो कि अभिजात्य वर्ग से हैं"। इसलिए भारत का ज़मींदार वर्ग यह समझ चुका था कि उनकी पहचान और कर्तव्य यही है की वह अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफदारी करें, इस प्रकार वह भी अंग्रेजों के समर्थक हो गए।
B.12 सामाजिक सुधार के प्रति रवैया
रूढ़िवादी वर्गों के साथ गठबंधन की नीति के रूप में, ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधारकों को सहायता पहुँचाने की नीति को त्याग दिया। उनका मानना था कि सन् 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई समाज सुधार की नीतियां - जैसे सती प्रथा पर रोक एवं विधवाओं का पुर्नविवाह थी। अतः उन्होंने धीरे-धीरे समाज सुधारकों को समर्थन देना बंद किया एवं रूढ़िवादी सोच का साथ दिया।
 जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ‘‘भारत एक खोज़’’ में व्यक्त किया ’’चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य का यह स्वभाविक समर्थन भारत में प्रतिक्रियावादियों की तरफ था, अतः वह भारत में प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ एवं आचरण का पालक एवं समर्थक था, जिसकी वे वैसे तो निंदा करते थे’’। वास्तव में ब्रिटिश सरकार एक दुविधा की अवस्था में थी। यदि ब्रिटिश समाज सुधार के पक्ष में जाते और उस हेतु अनेक कानून-कायदे जारी करते, तो रूढ़िवादी भारतीय उनके विरूद्ध जाते और कहते कि विदेशी सरकार को भारतीयों के आंतरिक, सामाजिक प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि वे इस प्रकार के कानून-कायदे जारी नहीं करते तो सामाजिक रूप से प्रगतिशील भारतीय इस तथ्य की निंदा करते कि सरकार समाजिक बुराईयों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक प्रश्नों में कदापि निष्पक्ष नहीं थी। यथास्थिति का साथ देकर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलित सामाजिक बुराईयों का संरक्षण करती थी। हालांकि राजनैतिक उद्देश्यों के लिये जातीयता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर ब्रिटिश सामाजिक प्रतिक्रिया को सक्रिय तरीके से प्रोत्साहन देते थे।
जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ‘‘भारत एक खोज़’’ में व्यक्त किया ’’चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य का यह स्वभाविक समर्थन भारत में प्रतिक्रियावादियों की तरफ था, अतः वह भारत में प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ एवं आचरण का पालक एवं समर्थक था, जिसकी वे वैसे तो निंदा करते थे’’। वास्तव में ब्रिटिश सरकार एक दुविधा की अवस्था में थी। यदि ब्रिटिश समाज सुधार के पक्ष में जाते और उस हेतु अनेक कानून-कायदे जारी करते, तो रूढ़िवादी भारतीय उनके विरूद्ध जाते और कहते कि विदेशी सरकार को भारतीयों के आंतरिक, सामाजिक प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि वे इस प्रकार के कानून-कायदे जारी नहीं करते तो सामाजिक रूप से प्रगतिशील भारतीय इस तथ्य की निंदा करते कि सरकार समाजिक बुराईयों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक प्रश्नों में कदापि निष्पक्ष नहीं थी। यथास्थिति का साथ देकर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलित सामाजिक बुराईयों का संरक्षण करती थी। हालांकि राजनैतिक उद्देश्यों के लिये जातीयता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर ब्रिटिश सामाजिक प्रतिक्रिया को सक्रिय तरीके से प्रोत्साहन देते थे।B.13 सामाजिक सेवा में चरम पिछड़ापन
19वीं सदी के दौरान जहाँ यूरोप में शिक्षा, स्वच्छता, जन-स्वास्थ्य, जल वितरण एवं ग्रामीण सड़कों जैसी सामाजिक सेवाओं ने तेजी से प्रगति दिखाई, भारत में ये अत्यंत पिछडे़पन की अवस्था में थे। तत्कालीन भारतीय सरकार ने प्राप्त आय का अधिकांश हिस्सा सेना, युद्ध एवं प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च किया और सामाजिक सेवा को धन से वंचित किया। उदाहरणार्थ 1886 में रूपये 47 करोड़ कुल राजस्व में से भारतीय सरकार ने लगभग रूपये 19.41 करोड़ सेना, में और रूपये 17 करोड़ नागरिक प्रशासन में खर्च किया परन्तु रूपये 2 करोड़ से कम शिक्षा, दवाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया एवं केवल 65 लाख रूपये सिंचाई पर खर्च किये। जो कुछ गिने-चुने कदम सेवाएं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करने हेतु उठाये गये थे, वे शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे और वे भी सिविल लाईन या ब्रिटिश या शहर के आधुनिक भाग पर केंद्रित थे। वे मुख्यतः यूरोपीय निवासी एवं गिने-चुने उच्च स्तर भारतीयों के लिये - जो शहरों के यूरोपीय भाग मे निवास करते थे - उनके लिए लागू थे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
B.14 श्रम विधान (Labour legislation)
19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों में श्रमिकों की हालत दयनीय थी। उन्हें नित्य 12-16 घंटे तक काम करना पड़ता था एवं कोई साप्ताहिक अवकाष नहीं था। महिलाएं एवं बच्चे भी लंबे समय तक काम करते थे जैसे पुरुष करते थे। उनका मासिक पारिश्रमिक अत्यंत कम था (प्रतिमाह रू. 4 से 20 के बीच)। कारखाने में अत्यधिक श्रमिक कार्यरत थे, कारखानों में प्रकाश एवं हवा की उचित व्यवस्था नहीं थी और स्थितियां स्वास्थ्य के प्रतिकूल थीं। मशीन पर काम करना जोखिम भरा था एवं दुर्घटनाएं होना आम बात थी।
भारतीय सरकार, जो पूंजीवादी की ओर झुकी थी, ने (अपर्याप्त) कदम उठाये ताकि आधुनिक कारखाने जिनके मालिक भारतीय थे, उनमें कार्य करने की दयनीय स्थिति में सुधार आये। इनमें मानवीय आधार आंषिक ही था। ब्रिटेन के निर्माताओं ने निरंतर दबाव डाला ताकि फैक्ट्री कानून जारी हो सकें। उन्हें भय था कि सस्ती मजदूरी के जरिये भारतीय निर्माता भारतीय बाजार में उनसे कहीं ज्यादा विक्रय करेंगे। वर्ष 1881 में प्रथम भारतीय फैक्ट्री एक्ट जारी किया गया।
- [col]
- यह कानून मुख्यतः बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। यह विधान किया गया कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे 9 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे। बच्चों को माह में चार दिनों का अवकाष दिया जावेगा। इस कानून में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि हानि पहुँचाने वाले यंत्र को बराबर सुरक्षित क्षेत्र में रखा जावे। वर्ष 1891 में द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम जारी किया गया। इससे सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया। महिलाओं का कार्य समय 11 घंटे प्रतिदिन रखा गया जबकि बच्चों का दैनिक कार्य समय घटाया गया। पुरुषों के लिये कार्य के समय में कोई संशोधन नहीं था।
- ब्रिटिश आधिपत्य में चाय व काॅफी के बागानों पर ये कानून लागू नहीं थे। अपितु सरकार ने विदेशी बागान मालिकों को हर प्रकार की सहायता दी जिससे कर्मचारियों का बहुत कठोर तरीके से शोषण हो सके। अधिकतर चाय बागान असम में स्थित थे जहाँ आबादी बहुत कम थी एवं मौसम स्वास्थ्य के प्रतिकूल था। अतः बागान में कार्य करने हेतु श्रमिक बाहर से आते थे परन्तु बागानों के मालिक बाहर से आये श्रमिकों को अधिक वेतन के द्वारा आकर्षित नहीं करते थे।
- बल्कि कपट एवं जोर-ज़बर्दस्ती से वे इन्हें नियुक्त करते थे एवं एक तरह से बागानों में गुलाम बनाते थे। भारतीय सरकार ने इन मालिकों को पूर्ण सहायता दी एवं वर्ष 1863, 1865, 1870, 1873 एवं 1882 में कठोर कानून जारी किये। एक बार किसी श्रमिक ने काम करने का अनुबंध किया, उसके पश्चात वो काम करने से मना नहीं कर सकता था। मजदूरों द्वारा अनुबंध का उल्लघंन एक आपराधिक जुर्म था तथा मालिक को ऐसे मजदूर को हिरासत में लेने का अधिकार था।
बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन अभियान के दबाव में आकर बेहतर मजदूर कानून 20वीं शताब्दी में जारी किये गये। फिर भी भारतीय मजदूर वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। एक औसत कर्मचारी ब्रिटिश साम्राज्य में निर्धारित स्तर के नीचे जीवनयापन करता था। भारतीय मजदूरों की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रो. जुर्गन कुग्ज़ीनस्की (जाने माने जर्मन आर्थिक इतिहासकार) ने 1938 में वर्णन किया किः ‘‘कम खाना खाकर, जानवरों की तरह कैद रहकर, बिना रोशनी व हवा व पानी के, भारतीय औद्यौगिक मजदूर विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे शोषित वर्ग है।’’
B.15 प्रेस पर प्रतिबंध
 ब्रिटिश सरकार भारत में प्रिटिंग प्रेस लाई एवं इस तरह आधुनिक प्रेस का विकास प्रारंभ किया। शिक्षित भारतीयों ने प्रेस की महत्ता को भांपा जिससे प्रेस सार्वजनिक विचार एवं सरकारी नीतियों की आलोचना से संबंधित जनचेतना में अहम् भूमिका निभा सकती थी। राम मोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोज़ी, जस्टिस रानाड़े, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, जी. सुब्रहमण्यम् अय्यर, सी. करूणाकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अन्य भारतीय नेताओं ने एक अहम् भूमिका निभाई जब उन्होंने समाचार पत्र प्रकाषित किये और उन्हें सशक्त राजनैतिक बल का रूप दिया। प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बन गया।
ब्रिटिश सरकार भारत में प्रिटिंग प्रेस लाई एवं इस तरह आधुनिक प्रेस का विकास प्रारंभ किया। शिक्षित भारतीयों ने प्रेस की महत्ता को भांपा जिससे प्रेस सार्वजनिक विचार एवं सरकारी नीतियों की आलोचना से संबंधित जनचेतना में अहम् भूमिका निभा सकती थी। राम मोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोज़ी, जस्टिस रानाड़े, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, जी. सुब्रहमण्यम् अय्यर, सी. करूणाकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अन्य भारतीय नेताओं ने एक अहम् भूमिका निभाई जब उन्होंने समाचार पत्र प्रकाषित किये और उन्हें सशक्त राजनैतिक बल का रूप दिया। प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बन गया।
भारतीय प्रेस से प्रतिबंध 1835 में चाल्र्स मेटकाल्फ् ने हटाए थे। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने स्वागत कर, ब्रिटिशराज का समर्थन किया था। किन्तु राष्ट्रवादियों ने धीरे-धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनचेतना जागृति हेतु किया। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रोधित होकर 1878 में ‘‘स्थानीय भाशाई प्रेस कानून’’ लागू किया। इस बंदिश का घोर विरोध हुआ और 1882 में इस कानून को खारिज कर दिया गया। अगले 25 वर्शाें तक प्रेस को काफी स्वतंत्रता मिली किन्तु 1905 में उग्र स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के कारण पुनः दमनकारी प्रेस कानून 1908 व 1910 में लाए गये।
B.16 नस्लीय घृणा (Racial antagonism)
 भारत में ब्रिटिश भारतवासियों से सदा दूरी रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक दूरी से वे भारत पर नियंत्रण एवं शासन बनाए रख सकते हैं। नस्ल के आधार पर वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। 1857 की बगावत (प्रथम स्वाधीनता युद्ध) एवं दोनों तरफ से किये गये अत्याचार के कारण ब्रिटिश एवं भारतीय नागरिकों के बीच में फासला बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरेआम नस्लीय सर्वोच्चता का तत्व आचरण में लाते थे और नस्लीय आधार पर अहंकार दिखाते थे। रेल्वे डिब्बों, रेल्वे स्टेशन में, प्रतीक्षालयों, पार्कों, होटलों, स्वीमिंग पूल इत्यादि में ‘‘केवल यूरोपीयों के लिए आरक्षित’’ उनके नस्लवाद का प्रमाण था। भारतीय अपमानित महसूस करते थे। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों मेंः
भारत में ब्रिटिश भारतवासियों से सदा दूरी रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक दूरी से वे भारत पर नियंत्रण एवं शासन बनाए रख सकते हैं। नस्ल के आधार पर वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। 1857 की बगावत (प्रथम स्वाधीनता युद्ध) एवं दोनों तरफ से किये गये अत्याचार के कारण ब्रिटिश एवं भारतीय नागरिकों के बीच में फासला बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरेआम नस्लीय सर्वोच्चता का तत्व आचरण में लाते थे और नस्लीय आधार पर अहंकार दिखाते थे। रेल्वे डिब्बों, रेल्वे स्टेशन में, प्रतीक्षालयों, पार्कों, होटलों, स्वीमिंग पूल इत्यादि में ‘‘केवल यूरोपीयों के लिए आरक्षित’’ उनके नस्लवाद का प्रमाण था। भारतीय अपमानित महसूस करते थे। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों मेंः ‘‘हम भारत में ब्रिटिश सम्राज्य के आरंभ से ही नस्लवाद के सभी रूप को जान गये हैं। इस शासन की संपूर्ण विचारधारा, 'हेरनवाॅक' (एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ है शासक जाति), और शासन का ढ़ांचा इसी विचारधारा पर आधारित है। ये बिना हिचकिचाए शासकों द्वारा घोषित था। षब्द से ज्यादा प्रभावशाली शासकों का आचरण था। पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्ष दर वर्ष भारत राष्ट्र एवं भारतीय नागरिक अपमान एवं शोषण के शिकार थे। अंग्रेज एक शाही समूह थे, हमे यह बताया गया, जिन्हें हम पर शासन करने के लिये ईश्वरीय हक प्राप्त था। यदि हम विद्रोह करते जो हमें याद दिलाया जाता था कि ‘शाही समूह के बाघ के गुण’ क्या हैं!’’
B.17 विदेश नीति
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, भारत ने अपने पड़ोसी देशों से नये आधार पर संबंधों का विकास किया। यह दो कारकों का परिणाम था। संचार के आधुनिक साधनों के विकास और देश के राजनैतिक व प्रशासनिक समेकलन ने भारत सरकार को भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक पहुँचने के लिये प्रेरित किया। यह रक्षा व आंतरिक एकता, दोनों के लिये आवश्यक था। यह निश्चित रूप से सीमा संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। दुर्भाग्यवश कभी-कभी भारत सरकार प्राकृतिक और पारंपरिक सीमाओं के परे चली गई। अन्य नया पहलू भारत सरकार का विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति, गुलाम देश की विदेश नीति से भिन्न होती है। स्वतंत्र राष्ट्र के मामले में यह देश के लोगों की ज़रूरतों व हितों पर आधारित होती हैं, अन्यथा यह शासक देश के हितों के लिये काम करती है। भारत के मामले में, विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थी। एशिया और अफ्रिका में ब्रिटिश सरकार के दो मुख्य उद्देश्य थेः उनके भारतीय साम्राज्य का संरक्षण एवं अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश वाणिज्य एवं आर्थिक व्यवसाय का विस्तार। इन दो उद्देश्यों हेतु ब्रिटिश साम्राज्य एवं आक्रमण भारत के सीमाओं के बाहर भी हुआ था। हालांकि इन्हीं उद्देश्यों के कारण ब्रिटिश सरकार का युद्ध अन्य यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ हुआ जो अपने प्रांतीय एवं वाणिज्य विस्तार अफ्रीका एवं एशिया में स्थित स्थानों पर चाहते थे। ऐसे अनेक संघर्षों की बात हमने विश्व इतिहास विषय में की है। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
भारतीय साम्राज्य की रक्षा, ब्रिटिश आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं अन्य यूरोपीय ताकतों को भारत की सीमा से दूर रखना - इन लक्ष्यों ने ब्रिटिश भारत सरकार को भारत के पड़ोसी राष्ट्रों पर हमला करने के लिये मजबूर किया। अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के समय, भारत के अपने पड़ोसी देश से संबंध ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आवश्यकताओं पर निर्भर थे।
परन्तु, यद्यपि भारतीय विदेशी नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुसार थी, उसकी कीमत भारत को ही चुकानी पडी़। ब्रिटिश उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु भारत को उसके पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करने पडे़; भारतीयों सैनिकों ने अपना खून अर्पित किया। भारतीय करदाता को इसकी कीमत चुकाना पड़ी।
 नेपाल के साथ युद्ध, 1814: अपने भारतीय साम्राज्य का भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तार करने की ब्रिटिश आकांक्षा के कारण सर्वप्रथम उत्तर में स्थित नेपाल साम्राज्य से युद्ध छिड़ा। अक्टूबर 1814 में दोनों राष्ट्रों की सीमा पुलिस दल की झड़पों से भारी युद्ध उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश नेपाल से अपेक्षाकृत मानव संसाधन, पैसे एवं सामग्री में सशक्त थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटिश षर्त के अनुसार शांति की संधि बनाना पड़ी। नेपाल ने ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ को स्वीकार किया। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जिलों को ब्रिटिश सरकार को सौंपा एवं तराई क्षेत्र में हक समर्पित किया। वे सिक्किम क्षेत्र से भी हटे। ब्रिटिश सरकार के लिये यह समझौता बहुत ही फायदेमंद रहा। भारतीय साम्राज्य की सीमा हिमालय तक पहुँच गई। मध्य-एशिया के साथ व्यवसाय संबंधी सुविधाओं से ब्रिटिश सरकार लाभान्वित हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल के लिये स्थल प्राप्त हुये। इसके अलावा गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिक संख्या में प्रवेश कर उसे मजबूत बनाया।
नेपाल के साथ युद्ध, 1814: अपने भारतीय साम्राज्य का भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तार करने की ब्रिटिश आकांक्षा के कारण सर्वप्रथम उत्तर में स्थित नेपाल साम्राज्य से युद्ध छिड़ा। अक्टूबर 1814 में दोनों राष्ट्रों की सीमा पुलिस दल की झड़पों से भारी युद्ध उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश नेपाल से अपेक्षाकृत मानव संसाधन, पैसे एवं सामग्री में सशक्त थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटिश षर्त के अनुसार शांति की संधि बनाना पड़ी। नेपाल ने ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ को स्वीकार किया। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जिलों को ब्रिटिश सरकार को सौंपा एवं तराई क्षेत्र में हक समर्पित किया। वे सिक्किम क्षेत्र से भी हटे। ब्रिटिश सरकार के लिये यह समझौता बहुत ही फायदेमंद रहा। भारतीय साम्राज्य की सीमा हिमालय तक पहुँच गई। मध्य-एशिया के साथ व्यवसाय संबंधी सुविधाओं से ब्रिटिश सरकार लाभान्वित हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल के लिये स्थल प्राप्त हुये। इसके अलावा गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिक संख्या में प्रवेश कर उसे मजबूत बनाया। बर्मा के साथ युद्धः 19 वीं शताब्दी के दौरान लगातार तीन युद्धों के द्वारा बर्मा का स्वाधीन साम्राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। बर्मा और ब्रिटिश भारत के बीच युद्ध सीमान्त संघर्ष द्वारा शुरू हुआ। साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से इस युद्ध को प्रोत्साहन मिला। अनेक वन संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की नजर थी। बर्मा में वे अपने व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार फ्रांसीसी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक प्रभाव का प्रसार बर्मा एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य भागों में होना रोकना चाहती थी।
- [col]
- 18वीं शताब्दी के समापन में बर्मा और ब्रिटिश भारत की एक समान सीमा का निर्माण हुआ, जब दोनों बढ़ती हुई ताकत थे। शताब्दियों के आंतरिक युद्ध के बाद बर्मा सन् 1752-1760 के बीच राजा अॅलान्गपाया द्वारा एकीकृत हुआ। उनके उत्तराधिकारी बाॅडवपाया जो एवा नदी (एरावदी के तट पर) स्थित शासन करते थे, सियाम पर लगातार आक्रमण किये, चीन आक्रमणों को विफल किया और सीमान्त प्रांतों जैसे अराकान (1785) एवं मणिपुर (1813) पर आक्रमण कर उन्हें जीता व बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत के पास लाया। पष्चिमी सीमा विस्तार करते हुए वह असम व ब्रम्हपुत्र घाटी के समीप तक आया। अंततः 1822 में बर्मा ने असम पर आक्रमण किया। अराकान और असम में बर्मा की आबादी के कारण बंगाल और बर्मा के बीच अनिर्मित सीमाओं पर लगातार क्लेश बना रहा।
- 1824 में ब्रिटिश शासन ने बर्मा पर आक्रमण किया। प्रारंभिक बाधा के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने बर्मा के सैनिकों को असम, कच्छर, मणिपुर व अराकान से भगाया। मई 1824 में ब्रिटिश सेना ने समुद्र द्वारा रंगून पर कब्जा किया और एवा स्थित राजधानी के 72 कि.मी. करीब आ गये। येंडबो के समझौते, जो फरवरी 1826 में किया गया, के जरिय़े शांति स्थापित हुई। बर्मा की सरकार ने (1) 1 करोड़ रूपये युद्ध मुआवजा के रूप में दिया, (2) अराकान और टेनासेरिम जैसे तटवर्ती प्रांत को समर्पित किया, (3) असम, कच्छर और जामतिया क्षेत्र में दावा छोड़ दिया, (4) मणिपुर को एक स्वाधीन प्रांत माना, (5) ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक समझौता किया, तथा (6) एवा में ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ का होना और कलकत्ता में एक बर्मा का प्रतिनिधित्व होना स्वीकार किया। इस समझौते के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बर्मा शासन को उनके तटवर्तीय प्रांतों से अलग किया और आने वाले समय में विस्तार हेतु बर्मा में एक ठोस आधार बनाया।
द्वितीय बर्मा युद्ध (1852) : ब्रिटेन के वाणिज्यिक लालच का परिणाम था। ब्रिटेन के लकड़ी के व्यापारी उत्तरी बर्मा में स्थित लकड़ी संसाधन पर रूचि दिखाने लगे। ब्रिटेन के लिये बर्मा की भारी आबादी एक विषाल बाजार के रूप में दिखने लगी, जहाँ ब्रिटिश कपासी सामग्री और अन्य वस्तुओं का विक्रय हो सके। ब्रिटेन जो कि बर्मा के दो तटवर्तीय प्रांतों में शासन कर रहा था, अब षेश प्रांतों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाना चाहता था। वह बर्मा के साथ युद्ध या शांति के द्वारा अपना कब्ज़ा मजबूत करना चाहता था ताकि उनके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी - जैसे फ्रांस और अमेरिका - वहां स्थापित न हो सकें। अप्रैल 1852 में एक पूर्ण ब्रिटिश सेना की नियुक्ति बर्मा में हुई। इस बार 1824-1826 की अपेक्षाकृत युद्ध कम समय के लिये रहा और ब्रिटेन की विजय और असरदार रही। ब्रिटिश सरकार ने पेगु, जो कि बर्मा का बचा हुआ तटवर्ती प्रांत था, कब्जे में लिया। परन्तु 3 साल तक इस शासन का विरोध रहा। तत्पश्चात दक्षिणी बर्मा को ब्रिटिश शासन के अधीन लाया गया। ब्रिटेन ने बर्मा के समस्त तटवर्ती इलाकों एवं समुद्र व्यवसायों पर कब्ज़ा किया। इस युद्ध का तमाम आर्थिक भार भारत द्वारा वहन किया गया।
पेगु के आक्रमण पश्चात बर्मा और ब्रिटेन के बीच संबंध बहुत सालों तक शांतिपूर्ण रहे। ब्रिटिश सरकार उत्तरी बर्मा को और खोलने हेतु प्रयासरत रही। विशेषकर ब्रिटिश व्यापारी व उद्योगपति बर्मा द्वारा चीन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाये रखने के प्रति आकर्शित रहे। 1885 में राजा थीबाॅ ने फ्रांस के साथ वाणिज्यिक समझौता किया। बर्मा में बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव से ब्रिटिश बहुत नाराज़ थे। ब्रिटिश व्यापारियों को यह भय था कि उनके फ्रेंच व अमेरिकन विपक्षी, धनी बर्मी मार्केट पर कब्जा करेगें। ब्रिटेन के वाणिज्यिक कक्ष एवं ब्रिटिश व्यापारी जो रंगून में स्थित थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उत्तरी बर्मा पर कब्जा करने के लिये दबाव डाला। 13 नवम्बर 1885 को ब्रिटिश सरकार ने बर्मा पर आक्रमण किया। 28 नवम्बर 1885 को राजा थीबाॅ ने आत्म समर्पण किया और तत्पश्चात उनके राजक्षेत्र भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिए गये।
परन्तु जिस सहजता से बर्मा पर कब्जा हुआ, वह चिर-स्थायी नहीं रहा। बर्मा की सेना के देशभक्त सैनिकों एवं अधिकारियों ने आत्म-समर्पण से इन्कार किया और घने जंगलों में चले गये। वहां से वे गुप्त तरीकों से आक्रमण करने लगे। उत्तरी बर्मा के नागरिक भी बगावत में खड़े हो गये। ब्रिटिश सरकार को 5 साल के लिये 40 हजार सैनिकों को भेजना पड़ा जिससे यह बगावत दबाई जा सके। इस युद्ध के संपूर्ण खर्चे भी भारत को वहन करना पड़े।
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बर्मा में एक आधुनिक वृहद राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बड़े पैमाने पर एक अभियान का आयोजन हुआ और गृह शासन की मांग रखी गई। बर्मा के देशभक्त भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ जुड़ गये। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने हेतु बर्मा को भारत से अलग किया। बर्मा के नागरिकों एवं नेताओं ने इस कदम का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यू आँग सान के नेतृत्व में बर्मा का राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा तक पहुँच चुका था। अंत में बर्मा को 4 जनवरी 1948 को आजादी प्राप्त हुई।
 अफगानिस्तान के साथ संबंध : अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के साथ दो युद्ध लडे़। ब्रिटेन के दृष्टिकोण में अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। भारत की सीमा के बाहर अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जहां रूस की ओर से खतरे पर रोक लगाई जा सकती थी एवं मध्य एशिया में ब्रिटेन के वाणिज्यिक उद्देश्य को सशक्त बनाया जा सकता था। यदि कुछ भी नहीं तो कम से कम दो विरोधी ताकतों के बीच अफगानिस्तान एक सहज केन्द्र के रूप में कार्य कर सकता था। ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव कमजोर होकर समाप्त हो पर अफगानिस्तान को वह एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर और विभाजित राष्ट्र हो जिस पर वे आसानी से नियंत्रण कर सकें।
अफगानिस्तान के साथ संबंध : अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के साथ दो युद्ध लडे़। ब्रिटेन के दृष्टिकोण में अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। भारत की सीमा के बाहर अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जहां रूस की ओर से खतरे पर रोक लगाई जा सकती थी एवं मध्य एशिया में ब्रिटेन के वाणिज्यिक उद्देश्य को सशक्त बनाया जा सकता था। यदि कुछ भी नहीं तो कम से कम दो विरोधी ताकतों के बीच अफगानिस्तान एक सहज केन्द्र के रूप में कार्य कर सकता था। ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव कमजोर होकर समाप्त हो पर अफगानिस्तान को वह एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर और विभाजित राष्ट्र हो जिस पर वे आसानी से नियंत्रण कर सकें।
ब्रिटिश सरकार दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान का एक स्वाभिमानी शासक था, को हटाना चाहती थी और उसके स्थान पर एक अधीनस्थ शासक को रखना चाहती थी। उन्होनें शाह शुजा को चुना जिन्हें 1809 में अफगान सीमा से हटाया गया था और जो अब लुधियाना में ब्रिटिश पेंशनर के रूप में निवास कर रहा था। अतः बिना कारण ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में दखल देने का निर्णय लिया और अफगानिस्तान पर कब्जा किया - फरवरी 1839 में। अफगान के मूल कबीलाईयों को रिश्वत द्वारा ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया था। 7 अगस्त 1839 को काबुल ब्रिटिश सरकार के अधीन आया और शाह षुजा को तत्काल अफगान शासन में विराजित किया गया। लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों ने शाह षुजा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे विदेशी सहायता के साथ अफगानिस्तान के राजा बने। बहुत से अफगान गुट विरोध में खड़े हो गये। 2 नवम्बर 1841 को एक बगावत हुई और अफगान सैनिकों ने ब्रिटिश ताकत का विरोध किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
11 दिसम्बर 1841 को ब्रिटिश सरकार ने अफगान प्रधानों के साथ एक समझौता किया जिसके तहत् उन्होंने दोस्त मोहम्मद को पुनः अफगानिस्तान का शासक बनाया। जब ब्रिटिश सैनिक वापस लौट रहे थे, उन पर आक्रमण हुआ। 16 हज़ार सैनिकों में से केवल 1 ही व्यक्ति सीमा पर जीवित पहुँचा। कुछ शेष, बंदियों के रूप में जीवित रहे। अंततः अफगानिस्तान पर युद्ध विफलता में परिणीत हुआ। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अब एक नई व्यूह रचना बनाई। 16 सितम्बर 1842 को काबुल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः कब्जा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस बार पिछली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ समझौता किया जिसके तहत् ब्रिटिश काबुल से विरक्त हुये और उन्हें (दोस्त मोहम्मद को) अफगानिस्तान का स्वाधीन शासक माना गया।
प्रथम अफगान युद्ध भारत के लिये 1.5 करोड़ रूपये से अधिक मंहगा पड़ा और सेना के लगभग 20 हज़ार सैनिक हताहत हुए।
ब्रिटिश सरकार ने अब अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1868 में जब रूस फिर मध्य एशिया की तरफ बढ़ा (जब वह क्रीमियाई युद्ध में पराजित हुआ), ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को एक मजबूत मध्य केन्द्र (बफर) बनाने की नीति अपनाई। काबुल के अमीर को सहायता एवं राहत प्रदान की गई और उनके विरोधियों को नियंत्रित करने एवं विदेशी विपक्षों से स्वाधीनता हेतु सहायता दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश के न हस्तक्षेप करने की नीति एवं समय समय पर सहायता देने से अमीर को रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने से रोका गया।
1870 के पश्चात संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद का पुर्नजागरण हुआ। रूस और ब्रिटेन के बीच झगड़े की बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को प्रत्यक्ष राजनैतिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया जिससे कि मध्य एशिया में ब्रिटेन का विस्तार संभव हो। अफगानिस्तान के शासक षेर अली पर ब्रिटिश नीति लागू करने हेतु 1878 में युद्ध छेड़ा गया जिसे द्वितीय अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1879 में शांति स्थापित हुई जब याकूब खान (षेर अली के पुत्र) का ने गंदामक समझौता किया जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को वो सब हासिल हुआ जो वे चाहते थे। उन्होंने कुछ सीमावर्ती जिलों को प्राप्त किया, काबुल में एक ‘रेसिडेंट’ रखने का हक प्राप्त किया एवं अफगानिस्तान की विदेशी नीति पर नियंत्रण संभव हो सका।
 परन्तु ब्रिटेन सरकार की यह कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं रही। अफगान नागरिकों के राष्ट्रीय गौरव पर आँच आई और अपनेस्वाधीनता की रक्षा हेतु वे आक्रमण पर उतरे। 3 सितम्बर 1879 को मेज़र कैवगनारी (ब्रिटिश रेसिडेंट) एवं उसके सषस्त्र सहायकों पर बागी अफगान सैनिकों द्वारा आक्रमण हुआ। इसमें उसकी मृत्यु हुई। अफगानिस्तान पर पुनः आक्रमण व कब्जा हुआ पर इस बार अफगानी अपना हुनर दिखा चुके थे। ब्रिटेन सरकार ने अपनी नीति को परिवर्तित किया और एक प्रबल और मैत्रीपूर्ण अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अब्दुर रहमान (दोस्त मोहम्मद के पौते) को अफगानिस्तान के नये शासक के रूप में माना गया। बदले में अब्दुर रहमान ने तय किया कि ब्रिटिश हुकुमत के अलावा किसी अन्य हुुकुमत के साथ राजनैतिक संबंध नहीं रखेगें। अतः अफगानिस्तान के अमीर अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण खो बैठे और उस हद तक परावलंबी शासक बने। साथ-साथ उन्होंने अपने राष्ट्र के आंतरिक मामलों पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
परन्तु ब्रिटेन सरकार की यह कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं रही। अफगान नागरिकों के राष्ट्रीय गौरव पर आँच आई और अपनेस्वाधीनता की रक्षा हेतु वे आक्रमण पर उतरे। 3 सितम्बर 1879 को मेज़र कैवगनारी (ब्रिटिश रेसिडेंट) एवं उसके सषस्त्र सहायकों पर बागी अफगान सैनिकों द्वारा आक्रमण हुआ। इसमें उसकी मृत्यु हुई। अफगानिस्तान पर पुनः आक्रमण व कब्जा हुआ पर इस बार अफगानी अपना हुनर दिखा चुके थे। ब्रिटेन सरकार ने अपनी नीति को परिवर्तित किया और एक प्रबल और मैत्रीपूर्ण अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अब्दुर रहमान (दोस्त मोहम्मद के पौते) को अफगानिस्तान के नये शासक के रूप में माना गया। बदले में अब्दुर रहमान ने तय किया कि ब्रिटिश हुकुमत के अलावा किसी अन्य हुुकुमत के साथ राजनैतिक संबंध नहीं रखेगें। अतः अफगानिस्तान के अमीर अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण खो बैठे और उस हद तक परावलंबी शासक बने। साथ-साथ उन्होंने अपने राष्ट्र के आंतरिक मामलों पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
प्रथम विश्व युद्ध एवं 1917 की रूसी क्रांति ने ब्रिटेन व अफगानिस्तान के बीच संबंधों में नई परेषानी खड़ी कर दी। अफगानों ने अब ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वाधीनता की मांग की। हबीबुल्लाह, जो अब्दुर रहमान के पश्चात 1901 से अफगानिस्तान का अमीर था, 20 फरवरी 1919 को मारा गया और उनके पुत्र अमानुल्लाह (अफगानिस्तान का नया अमीर) ने ब्रिटिश इंड़िया पर युद्ध घोषित किया। 1921 में समझौते के द्वारा शांति स्थापित हुई जिससे अफगानिस्तान ने विदेश मामलों में संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की।
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]
[next]
Lecture continues here ...
C. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
C.1 प्रस्तावना
भारत में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक जागृति पनपी और संगठित राष्ट्रीय आंदोलन फले-फूले। दिसम्बर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ जिसके नेतृत्व में भारतीयों ने एक लम्बा व साहसी संघर्ष किया जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को लंबे एवं दमनकारी विदेशी शासन से स्वतंत्रता मिली।
C.2 इनसे पहले कौन आये
 1870 तक ये स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर्याप्त शक्ति और गति के साथ राजनैतिक पटल पर दिखाई दे रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसम्बर 1885 में हुई जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। यद्यपि इसके कई पूर्ववर्तीय थे।
1870 तक ये स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय राष्ट्रवाद पर्याप्त शक्ति और गति के साथ राजनैतिक पटल पर दिखाई दे रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसम्बर 1885 में हुई जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति थी। यद्यपि इसके कई पूर्ववर्तीय थे।राजा राममोहन राय पहले भारतीय नेता थे जिन्होनें राजनैतिक सुधारों के लिये आन्दोलन चलाया। 1836 के बाद कई लोक संगठन, भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किये गये। ये सारे संगठन समकालीन 'सम्पन्न लोगों' द्वारा चलाये जाते थे किन्तु यह मुख्यतः स्थानीय या प्रांतीय स्तर के होते थे। इनका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, भारतीयों का प्रशासन के साथ संबंध, शिक्षा का प्रसार, भारतीयों की माँगों को ब्रिटिश संसद के सामने रखना, आदि होता था।
1858 के बाद के कालखण्ड में शिक्षित भारतीयों और ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के बीच दूरियाँ बढ़ती चली गयीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश राज की नींव हिला कर रख दी थी। जैसे-जैसे शिक्षित भारतीय वर्ग ने ब्रिटिश नीतियों एवं उससे भारत पर पढ़ने वाले परिणामों को समझा, वैसे-वैसे वे ब्रिटिश नीतियों के कटुतर आलोचक बनने लगे। धीरे-धीरे इस आलोचना को राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलने लगी। समकालीन राजनीतिक संगठन, राजनीतिक रूप से जागृत भारतीयों को ज्यादा संतुष्ट नहीं रख सके। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
 1866 में, दादाभाई नौरोजी ने, ब्रिटिश राजनेताओं को भारतीयों लोक कल्याण एवं भारत के प्रश्नों को उठाने के लिए, लन्दन में ‘ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन’ की स्थापना की। बाद में उन्होनें इस संगठन की शाखाओं का विस्तार भारतीय शहरों में भी किया। 1825 में जन्मे दादाभाई ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को समर्पित किया और शीघ्र ही वे भारत के पितामह (Grand old man) कहलाने लगे। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक व चिन्तक थे। अपने लेखन में उन्होनें दर्षाया कि भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण ब्रिटिश-षोशक नीतियाँ थी, जिसके कारण भारत का धन बाहर जा रहा था। दादाभाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तीन कार्यकाल मिले। वस्तुतः वे पहले ऐसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे जिनका लोग हृदय से सम्मान करते थे।
1866 में, दादाभाई नौरोजी ने, ब्रिटिश राजनेताओं को भारतीयों लोक कल्याण एवं भारत के प्रश्नों को उठाने के लिए, लन्दन में ‘ईस्ट-इण्डिया एसोसिएशन’ की स्थापना की। बाद में उन्होनें इस संगठन की शाखाओं का विस्तार भारतीय शहरों में भी किया। 1825 में जन्मे दादाभाई ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को समर्पित किया और शीघ्र ही वे भारत के पितामह (Grand old man) कहलाने लगे। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक व चिन्तक थे। अपने लेखन में उन्होनें दर्षाया कि भारतीय गरीबी का प्रमुख कारण ब्रिटिश-षोशक नीतियाँ थी, जिसके कारण भारत का धन बाहर जा रहा था। दादाभाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तीन कार्यकाल मिले। वस्तुतः वे पहले ऐसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे जिनका लोग हृदय से सम्मान करते थे।
कांग्रेस से पहले के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में इण्डियन एसोसिएशन आॅफ कलकत्ता था। बंगाल के युवा राष्ट्रवादी ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन की सामन्तोन्मुखी नीतियों से चिढ़ने लगे थे। वे वृहद् लोक कल्याण के लिये बड़ा राजनीतिक आंदोलन चाहते थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, जो कि एक बुद्धिमान लेखक एवं वक्ता थे, के रूप में उन्हें एक नेतृत्व मिला।
उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा से अन्यायपूर्ण तरीके से अपदस्थ कर दिया गया था क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी एक स्वतंत्र सोच वाले भारतीय को सहन नहीं कर सके थे। 1857 में कलकत्ता (आज कोलकात्ता) के छात्रों को एक राष्ट्रवादी उद्बोधन देते हुए उन्होनें अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत की। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और आनन्द मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने राजनीतिक मुद्दों पर भारतीयों की एकता और देश में दृढ़ राजनीतिक विचारों को तैयार करना, अपना लक्ष्य बनाया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने झण्डे तले लाने के लिए इन्होनें न्यूनतम सदस्यता शुल्क रखा। एसोसिएशन की कई शाखाएं बंगाल के शहरों एवं गाँवों के साथ-साथ बंगाल के बाहर भी प्रारंभ हुईं।
भारत के दूसरे हिस्सों में भी युवा सक्रिय थे। 1870 के दशक में, जस्टिस रानाडे और उनके साथियों ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1884 में एम.वीरराघवचारी, जी. सुब्रमण्यम अैयर, आनन्द चार्लु और साथियों ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। फिरोजशाह मेहता, के.टी. तेलंग, बद्रूद्दीन तैय्यबजी आदि ने 1885 में बाॅम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन की स्थापना की।
अब समय आ गया था कि सारे राष्ट्रवादी, जो विदेशी शासन व शोषण के विरूद्ध एकीकृत राजनैतिक आन्दोलन चाहते थे, एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच पर एक साथ आएं। समकालीन संगठन अपना कार्य पूरी निष्ठा से करने के बावजूद कई दृष्टिकोणों से संकीर्ण थे, क्योंकि वे स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और उनके सदस्य भी किसी विशेष शहर या प्रान्त से होते थे। यहाँ तक कि ‘इण्डियन एसोसिएशन’ भी अखिल भारतीय मंच नहीं बन सका।
C.3 इण्डियन नेशनल काँग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस) का आगमन
 कई भारतीय, राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजना बना रहे थे। किन्तु इसका श्रेय एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. हृयूम को जाता है, जिन्होंने इस विचार को अन्तिम रूप दिया। उन्होनें प्रमुख भारतीय नेताओं की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसम्बर 1885 में बाम्बे में सम्पन्न करवाया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता डबल्यू. सी. बैनर्जी ने की।
कई भारतीय, राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजना बना रहे थे। किन्तु इसका श्रेय एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. हृयूम को जाता है, जिन्होंने इस विचार को अन्तिम रूप दिया। उन्होनें प्रमुख भारतीय नेताओं की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसम्बर 1885 में बाम्बे में सम्पन्न करवाया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता डबल्यू. सी. बैनर्जी ने की।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश के विभिन्न हिस्सों के नेताओं के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, जाति, धर्म या प्रान्त के परे एक राष्ट्रीय भावना का विकास, लोगों की इच्छानुसार माँगे सरकार के सामने प्रस्तुत करना और इन सबसे महत्वपूर्ण देश में लोक-मत का निर्माण करना जैसे उद्देश्य पहले अधिवेशन में घोषित किये। यह भी कहा जाता है कि हृयूम का उद्देश्य, कांग्रेस को एक ऐसा संगठन बनाना था जो एक ‘‘सेफ्टी वाल्व’’ का कार्य करे और शिक्षित भारतीयों में पनप रहे ब्रिटिश विरोधी विचारों को उचित व सुरक्षित निकास मिले। हृयूम, असंतुष्ट राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों तथा असंतुष्ट व शोषित किसानों के किसी मिले-जुले संगठन बनने की संभावना को होने से रोकना भी चाहते थे।
 यह ‘सेफ्टी वाल्व’ सिद्धांत, पूर्ण सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपर्याप्त व भ्रमित करने वाला है। किसी भी दूसरे संगठन से ज्यादा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से जागृत उन भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया जो देश की राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए काम करना चाहते थे। शक्तिशाली तत्वों के सक्रिय होने के कारण भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा था। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक कि हृयूम के उद्देश्य भी मिले जुले थे। वास्तव में उनके उद्देश्य ‘सेफ्टी वाल्व’ की अपेक्षा ज्यादा साहसी थे। वह भारत और उसके किसानों से सच्चा प्यार करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखने में जिन नेताओं ने हृयूम की मदद की वे सच्चे देशभक्त तथा चरित्रवान लोग थे। उन्होने स्वेच्छा से हृयूम की मदद स्वीकारी क्योंकि वे अपने प्रयासों के प्रति, इस प्रारंम्भिक अवस्था में सरकार से कोई अनिवार्य शत्रुता भी नहीं चाहते थे और आशा करते थे कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी की सक्रियता सरकारी शक की तीव्रता को कम करेगी। यदि हृयूम कांग्रेस को एक ‘सेफ्टी वाल्व’ की तरह उपयोग करना चाहते थे तो प्रारम्भिक कांग्रेस नेता हृयूम को एक ‘तड़ित चालक’ के रूप में देख रहे थे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
यह ‘सेफ्टी वाल्व’ सिद्धांत, पूर्ण सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपर्याप्त व भ्रमित करने वाला है। किसी भी दूसरे संगठन से ज्यादा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से जागृत उन भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया जो देश की राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए काम करना चाहते थे। शक्तिशाली तत्वों के सक्रिय होने के कारण भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा था। किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक कि हृयूम के उद्देश्य भी मिले जुले थे। वास्तव में उनके उद्देश्य ‘सेफ्टी वाल्व’ की अपेक्षा ज्यादा साहसी थे। वह भारत और उसके किसानों से सच्चा प्यार करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखने में जिन नेताओं ने हृयूम की मदद की वे सच्चे देशभक्त तथा चरित्रवान लोग थे। उन्होने स्वेच्छा से हृयूम की मदद स्वीकारी क्योंकि वे अपने प्रयासों के प्रति, इस प्रारंम्भिक अवस्था में सरकार से कोई अनिवार्य शत्रुता भी नहीं चाहते थे और आशा करते थे कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी की सक्रियता सरकारी शक की तीव्रता को कम करेगी। यदि हृयूम कांग्रेस को एक ‘सेफ्टी वाल्व’ की तरह उपयोग करना चाहते थे तो प्रारम्भिक कांग्रेस नेता हृयूम को एक ‘तड़ित चालक’ के रूप में देख रहे थे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy अतः 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ, विदेशी शासन से मुक्ति के लिये संघर्ष छोटे किन्तु संगठित स्तर पर आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था और लोग आजादी मिलने तक चैन से नहीं बैठने वाले थे। काँग्रेस एक पार्टी ही नहीं वरन् आंदोलन की तरह चलने वाली थी। 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि देश के भिन्न-भिन्न स्थानीय संगठनों एवं समूहों से चुने गये। वर्ष में एक बार, प्रत्येक दिसम्बर में, देश के किसी नए शहर में नेषनल कांग्रेस की सभा होने लगी। शीघ्र ही प्रतिनिधियों की संख्या हजारों में हो गई जो सामान्यतः वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक और सामंती लोग थे। 1890 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया। यह इन अर्थों में प्रतीकात्मक था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय महिलाओं को उनकी शताब्दियों की पतित अवस्था से उपर लायेगा।
अतः 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ, विदेशी शासन से मुक्ति के लिये संघर्ष छोटे किन्तु संगठित स्तर पर आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था और लोग आजादी मिलने तक चैन से नहीं बैठने वाले थे। काँग्रेस एक पार्टी ही नहीं वरन् आंदोलन की तरह चलने वाली थी। 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि देश के भिन्न-भिन्न स्थानीय संगठनों एवं समूहों से चुने गये। वर्ष में एक बार, प्रत्येक दिसम्बर में, देश के किसी नए शहर में नेषनल कांग्रेस की सभा होने लगी। शीघ्र ही प्रतिनिधियों की संख्या हजारों में हो गई जो सामान्यतः वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षक और सामंती लोग थे। 1890 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया। यह इन अर्थों में प्रतीकात्मक था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय महिलाओं को उनकी शताब्दियों की पतित अवस्था से उपर लायेगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र माध्यम नहीं था जहाँ से राष्ट्रवादी धारा का प्रवाह हो रहा था। प्रांतीय सभाएँ, स्थानीय संगठन और राष्ट्रवादी समाचार पत्र बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य प्रमुख अंग थे। इनमें प्रमुख रूप से प्रेस बढ़ते राष्ट्रवादी विचारों एवं आंदोलन का सशक्त माध्यम था। निश्चित तौर पर, उस दौर के अधिकांश समाचार पत्र राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए स्थापित किये गये थे ना कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के तौर पर। दादाभाई नौरोजी, बदरूद्दीन तैय्यबजी, फिरोजशाह मेहता, पी. आनन्द चार्लु, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, रोमेशचन्द्र दत्त, आनन्द मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेता राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारम्भिक अध्यक्षों में से थे। इस दौर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बालगंगाधर तिलक, शिशिर कुमार व मोतिलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और दिनशॉ इ. वाचा, आदि शामिल थे।
C.4 प्रारम्भिक राष्ट्रवादी
प्रारम्भिक राष्ट्रवादी सोचते थे कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष अभी प्रमुख मुद्दा नहीं था। उस समय प्रमुख मुद्दे यह थे कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास व उनका सुदृढ़ीकरण कैसे हो, और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए। इस दिशा में पहला काम यह था कि आम लोगों को लोकहित में राजनीति गतिविधियों से जोड़ना था। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से जागृत लोगों व नेताओं की बीच राष्ट्रीय एकता स्थापित करना था। प्रारम्भिक राष्ट्रीय नेता इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे कि एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया की यह शुरूआत मात्र थी। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास सावधानीपूर्वक करना था। राजनीतिक रूप से जागृत नेताओं के लिए यह जरूरी था कि वे क्षेत्र, जाति या धर्म के परे, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सतत् रूप से काम करें। प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों द्वारा आर्थिक व राजनीतिक माँगे इस तरह तैयार की गई थी कि लोगों के एक समान आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम तैयार हो सके।
C.5 आर्थिक उपनिवेदशवाद की विवेचना (Economic imperialism's review)
प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होनें उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की। उन्होनें उपनिवेशिक आर्थिक शोषण के तीनों ही मुद्दों, व्यापार, उद्योग एवं वित्त को उठाया। उन्होनें ब्रिटिश शासन की उस कोशिश का जोरदार विरोध किया जिसमें अंग्रेज़ भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। औपनिवेशिक संरचना पर आधारित लगभग हर सरकारी नीति का सशक्त विरोध किया गया। राष्ट्रीयवादी ब्रिटेन की भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बनाने की तीनों कोशिशों का विरोध करने लगे - अर्थात् भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, ब्रिटिश माल का बाज़ार बनाना एवं विदेशी पूंजी निवेश का अड्डा बनाना। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
प्रारम्भिक राष्ट्रवादिओं ने भारत में बढ़ती गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, आधुनिक उद्योगों व कृषि के असफल होने की शिकायत की और इसके लिए ब्रिटिश आर्थिक शोषण को जिम्मेदार ठहराया। दादाभाई नौरोजी ने 1881 में ही घोषित किया कि अंग्रेज शासन, ‘‘हर दिन बढ़ता हुआ, कभी न खत्म होने वाला विदेशी आक्रमण है जो कि धीरे-धीरे देश को पूर्णतः नष्ट कर देगा’’। राष्ट्रवादियों ने भारत के परम्परागत हस्त शिल्प उद्योग को नष्ट करने वाली और आधुनिक उद्योगों के विकास को रोकने वाली सरकारी आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उनमें से अधिकांश ने भारतीय रेलवे, उद्योग व बागानों में विदेशी पूँजी निवेश का इस आधार पर विरोध किया कि यह भारतीय पूँजीवाद का अहित कर अन्ततः ब्रिटिश आर्थिक व राजनीतिक हितों को लाभ पहुचाएगा।
- [col]
- उनका विश्वास था कि विदेशी पूँजी निवेश न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिये एक गंभीर राजनीतिक एवं आर्थिक खतरा है बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करेगा। उनकी नजर में, भारत की गरीबी को दूर करने का प्रमुख तरीका था आधुनिक उद्योगों का तीव्र विकास। वे चाहते थे कि सरकारी मदद और कर छूटों के साथ, सरकार ही आधुनिक उद्योगों का विकास करे। उन्होने स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, लोगों से देशी सामान उपयोग करने का आव्हान किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उदाहरण के तौर पर 1896 में पूना व महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों में छात्रों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन को बल दिया।
- राष्ट्रवादियों की शिकायत यह थी कि भारतीय पूँजी का निर्गमन इंग्लैंड की ओर था और इसे तत्काल रोकने की जरूरत थी। उन्होंने भारतीय किसानों पर करों के बोझ को कम करने के लिए आन्दोलन किये। उनमें से कुछ ने अंग्रेजों की सामंतवादी प्रणाली की भी आलोचना की। राष्ट्रवादियों ने भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए भी आन्दोलन किये। उन्होनें उच्च कराधान को भारत में गरीबी का प्रमुख कारण मानते हुए ‘नमक कर’ को समाप्त करने और भूमिकर को कम करने की माँग की। उन्होने भारत सरकार के उचे रक्षा खर्चों की भी आलोचना की और इसे घटाने की माँग भी की। जैसे-जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे ज्यादातर राष्ट्रीय नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्थिक शोषण और गरीबी और इसके आर्थिक परिणाम, विदेशी शासन के लाभों की तुलना में कही ज्यादा घातक हैं।
इस प्रकार, जीवन व सुरक्षा के संबंध लाभों पर, टिप्पणी करते हुए दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि: ‘‘यह भ्रम है कि भारत में जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। एक अर्थ में ही जीवन व सम्पत्ति सुरक्षित है कि लोग आपसी हिंसा और स्थानीय राजाओं से सुरक्षित है, किन्तु अंग्रेजों की ओर से कोई सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए जीवन भी सुरक्षित नहीं है। भारत की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। केवल इंग्लैंड, भारत से कोसों दूर, 30,000,000 या 40,000,000 पाउण्ड धन प्रतिवर्ष खाकर पूर्णतः सुरक्षित है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ भारत में उसकी सम्पत्ति और जीवन सुरक्षित नहीं है। करोड़ों भारतीयों के लिए जीवन का सीधा अर्थ है - 'आधा भोजन या भूखमरी या अकाल और बीमारी'।’’
सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course
कानून और व्यवस्था के बारे में, दादाभाई कहते हैं: ‘‘एक भारतीय कहावत है, ‘किसी के पेट पर लात मत मारो, चाहे पीठ पर कितना भी मारो’। स्थानीय राजाओं के अधीन लोग अपनी फसलों का उपभोग करते थे, यद्यपि कभी-कभी उन्हे पीठ पर मार सहनी पड़ती थी। अंग्रेज शासन के अधीन, भारत में हिंसा नहीं है, शांति है केवल उसकी फसल व धन का अदृश्य, सूक्ष्म व शांतिपूर्ण तरीके से निर्गमन हो रहा है - वह भूख से मरता है, नष्ट होता है किन्तु शांति से, कानून एवं व्यवस्था के साथ!’’
आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण था कि भारत में अंग्रेज शासन शोषण पर आधारित था, जिसके कारण भारत में आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी एवं अधूरा विकास हो रहा था। इन नुकसानों ने भारत में ब्रिटिश शासन के तथाकथित फायदों को खत्म कर दिया था।
C.6 प्रारम्भिक राष्ट्रवादी नेताओं की गतिविधियाँ व कार्यक्रम

1905 स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उन नेताओं के हाथों में था जो उदारवादी या उदार राष्ट्रवादी माने जाते थे। उदारवादियों की राजनीतिक पद्धति को संवैधानिक आंदोलन कहा जा सकता है जो कानून की चार दीवारी में बन्द था। यह एक धीमा व क्रमिक राजनीतिक आन्दोलन था। उनका विश्वास था कि यदि लोक मत तैयार कर संगठित होकर याचिका, सभा, भाशणों आदि के माध्यम से अपनी बात रखी जाती है तो अंग्रेज क्रमबद्ध रूप से धीरे-धीरे उनकी माँगे मान लेगें।
इस प्रकार उनका राजनीतिक कार्य द्वि-दिशात्मक था। पहला, वे लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं राजनीतिक जागृति के लिये एक सशक्त लोकमत का निर्माण और लोगों को राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित कर एकत्र करना चाहते थे। आधारभूत रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव में भी इसी उद्देश्य को लेकर निर्देश थे। यद्यपि उनके ज्ञापन व याचिकाएँ सरकार को संबोधित करती प्रतीत होतीं थीं, किन्तु उनका वास्तविक उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना था। उदाहरण के लिए जब 1891 में पूना सार्वजनिक सभा द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किये गये ज्ञापन पर सरकार ने मात्र दो पंक्ति का उत्तर दिया तो युवा नेता गोखले ने अपनी हताषा व्यक्त की, तब न्यायमूर्ति रानाडे ने कहा: ‘‘तुम्हें, हमारे देश के इतिहास में हमारे स्थान का बोध नहीं है। ये ज्ञापन सामान्यतः सरकार को संबोधित होते हैं। वास्तव में तो ये जनता को संबोधित होते हैं ताकि वे सीख सकें कि इस दिशा में कैसे सोचा जा सकता है। ऐसा कार्य कई वर्षों तक करना आवश्यक है, वह भी परिणामों की आशा के बगैर क्योंकि इस भूमि पर इस तरह की राजनीति नई है।’’
 दूसरी बात यह थी कि राष्ट्रवादी नेता, ब्रिटिश सरकार और जनता को उन सुधारों के लिये समझाना चाहते थे, जिसमें राष्ट्रवादियों का भी दखल हो। उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता व संसद भारत के प्रति न्यायषील होना चाहते थे किन्तु उन्हें भारत की सही दषा का ज्ञान नहीं था। इसलिए, भारतीय लोकमत को जागृत करने के बाद उदारवादियों ने अपना ध्यान ब्रिटिश लोकमत की ओर दिया। इस उद्देश्य से उन्होनें ब्रिटेन में सक्रिय प्रचार कार्यक्रम चलाया। प्रमुख भारतीय नेताओं के प्रतिनिधि मण्डल, भारतीय दृष्टिकोण को समझाने के लिए ब्रिटेन भेजे गये। 1889, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया गया। 1890 में इस समिति ने एक समाचार पत्र ‘‘इण्डिया’’ का प्रकाशन प्रारम्भ किया। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन व आय का बड़ा हिस्सा इंग्लैण्ड में भारतीय पक्ष को समझाने में खर्च किया।
दूसरी बात यह थी कि राष्ट्रवादी नेता, ब्रिटिश सरकार और जनता को उन सुधारों के लिये समझाना चाहते थे, जिसमें राष्ट्रवादियों का भी दखल हो। उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता व संसद भारत के प्रति न्यायषील होना चाहते थे किन्तु उन्हें भारत की सही दषा का ज्ञान नहीं था। इसलिए, भारतीय लोकमत को जागृत करने के बाद उदारवादियों ने अपना ध्यान ब्रिटिश लोकमत की ओर दिया। इस उद्देश्य से उन्होनें ब्रिटेन में सक्रिय प्रचार कार्यक्रम चलाया। प्रमुख भारतीय नेताओं के प्रतिनिधि मण्डल, भारतीय दृष्टिकोण को समझाने के लिए ब्रिटेन भेजे गये। 1889, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया गया। 1890 में इस समिति ने एक समाचार पत्र ‘‘इण्डिया’’ का प्रकाशन प्रारम्भ किया। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन व आय का बड़ा हिस्सा इंग्लैण्ड में भारतीय पक्ष को समझाने में खर्च किया।
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का छात्र (अध्येता) जब उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार देखता है तो वह भ्रमित हो सकता है। इस वफादारी का कतई यह मतलब नहीं है कि वे सच्चे देशभक्त नहीं थे या ड़रपोक लोग थे। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन से सतत् राजनीतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण थे। इसलिए उन्होने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का नहीं बल्कि अंग्रेजों से सत्ता राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरण का उद्देश्य बनाया। बाद में उनमें से कईयों ने ब्रिटिश शासन की बुराई करते हुए, राष्ट्रीय सुधारों की माँग पूरी न करने का आरोप लगाते हुए भारत के लिए स्वराज्य की माँग की एवं ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी को तिलांजली दे दी। उनमें से कई नेता उदारवादी थे क्योंकि उनका मानना था कि अभी विदेशी सत्ता को प्रत्यक्ष चुनौती देने का सही समय नहीं आया है। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
C.7 बंगाल का विभाजन (The partition of Bengal)
 जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद की लहरें उठने लगी और स्वतंत्रता आंदोलन ने दूसरे दौर में प्रवेश किया।
जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद की लहरें उठने लगी और स्वतंत्रता आंदोलन ने दूसरे दौर में प्रवेश किया।
20 जुलाई 1905 को लाॅर्ड़ कर्ज़न ने बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित करने का आदेश जारी किया : एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे जिसकी जनसंख्या लगभग तीन करोड़ दस लाख थी, और दूसरा षेश बंगाल जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी (इनमें 1 करोड़ 8 लाख बंगाली और षेश बिहारी और उड़िया थे)। यह कहा गया कि तत्कालीन बंगाल प्रांत प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। हालांकि जिन अधिकारियों ने इस योजना को बनाया उनका राजनीतिक मंतव्य अलग था। उन्हें आशा थी कि यह कदम बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद के ज्वार को थाम लेगा क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का केन्द्र था। 06 दिसम्बर 1904 को भारत के गृह सचिव रिज़ली ने एक सरकारी नोट में लिखा कि: ‘‘एकीकृत बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग-अलग रास्तों पर चलेगा। यही वह तथ्य है जो कांग्रेसी नेता महसूस करते हैं। उनकी चिन्ता सही है, हमारा मुख्य उद्देश्य विरोधियों को विभाजित कर उन्हें कमजोर करना है।’’
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियोें ने बंगाल के विभाजन का तीव्र विरोध किया। बंगाल के भीतर ही समाज के विभिन्न वर्गों - जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, गरीब और यहा तक कि महिलाएँ भी उनके प्रान्त विभाजन के विरोध में स्वतः स्फूर्त खड़े हो गये।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियोें ने बंगाल के विभाजन का तीव्र विरोध किया। बंगाल के भीतर ही समाज के विभिन्न वर्गों - जमींदार, व्यापारी, वकील, छात्र, गरीब और यहा तक कि महिलाएँ भी उनके प्रान्त विभाजन के विरोध में स्वतः स्फूर्त खड़े हो गये।
राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए एक चुनौती माना न कि केवल एक प्रशासनिक कदम। उनके अनुसार यह एक सोची-समझी रणनीतिक चाल थी जिसमें बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके को पूर्वी बंगाल और हिन्दु बहुल क्षेत्र को पष्चिम बंगाल कहा गया था ताकि वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। यह बंगाली भाशा व संस्कृति के विकास में भी एक झटका होता। उन्होने दर्षाया कि प्रशासनिक क्षमता की दृष्टि से हिन्दी भाषी बिहार, उड़िया भाषी उड़िसा और बंगाल भाषी बंगाल में बाँटना बेहतर होता। इससे भी ज्यादा, प्रशासनिक कदम पूर्णतः लोक इच्छा के विरूद्ध उठाया गया। इस प्रकार विभाजन के विरूद्ध विरोध की तीव्रता की व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि यह संवेदनषील और साहसी भारतीयों पर एक प्रहार था।
C.8 विभाजन-विरोधी आन्दोलन
 विभाजन-विरोधी आन्दोलन, बंगाल के राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यों का परिणाम था न कि केवल एक समूह का। प्रारम्भिक दौर में इसका नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और कृश्णा कुुमार मित्रा जैसे उदारवादी नेताओं ने किया; उग्र राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी नेता बाद के दौर में इससे जुडे। वास्तव में, उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही प्रकार के नेताओं ने आंदोलन के दौरान एक दूसरे को सहयोग दिया।
विभाजन-विरोधी आन्दोलन, बंगाल के राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यों का परिणाम था न कि केवल एक समूह का। प्रारम्भिक दौर में इसका नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और कृश्णा कुुमार मित्रा जैसे उदारवादी नेताओं ने किया; उग्र राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी नेता बाद के दौर में इससे जुडे। वास्तव में, उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही प्रकार के नेताओं ने आंदोलन के दौरान एक दूसरे को सहयोग दिया।
विभाजन विरोधी आन्दोलन 7 अगस्त 1946 को प्रारम्भ हुआ। उस दिन कलकत्ता के ‘टाउन हाल’ में बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। इस सभा के बाद सारे प्रतिनिधि, आंदोलन को गति देने के लिये पूरे प्रान्त में फैल गये।
विभाजन 16 दिसम्बर 1905 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने इसे सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय षोक के रूप में घोषित कर विरोध किया। उस दिन भूख हड़ताल भी रखी गई। कलकत्ता में भी हड़ताल हुई, लोगों ने सुबह-सुबह नंगे पैर गंगा पहुंचकर, डुबकी लगाई। इस अवसर पर गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगौर ने ‘‘अमार सोनार बांग्ला’’ नामक गीत रचा जिसे लोग जुलूस के समय गलियों में गाते थे। यह गीत बांग्लादेश के द्वारा 1971 में उसकी मुक्ति के पश्चात, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। कलकत्ता की गलियाँ ‘वंदे मातरम्’ के घोष से गूँज उठी और यह शीघ्र ही राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख गीत बन गया। रक्षाबंधन के अवसर पर हिन्दू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बाँधकर अटूट एकता का संदेश दिया और इस तरह राखी का त्यौहार एक नए अर्थों में मनाया गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
दोपहर में जब, वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता आनन्द मोहन बोस ने फेड़रेशन हाॅल, जो बंगाल की अखण्ड़ता का प्रतीक था, की नींव रखी तो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। उन्होनें 50,000 से ज्यादा लोगों के समूह को संबोधित किया।
C.9 स्वदेशी और बहिष्कार
बंगाली नेताओं ने महसूस किया कि केवल प्रदर्शन, सभा, रैलियों या ज्ञापनों से शासकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए ज्यादा प्रभावी कदम, जो जनप्रिय भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सके, की जरूरत थी। इस समस्या का हल था: स्वदेशी और बहिष्कार। संपूर्ण बंगाल में सामूहिक सभाएँ आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग एवं विदेशी चीजों के बहिष्कार की घोषणा, षपथपूर्वक की गई। सार्वजनिक जगहों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन को बड़ी सफलता मिली। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के अनुसार: ‘‘अपने शीर्ष सफलता के दौर में, स्वदेशी ने हमारे पारिवारिक व सामाजिक जीवन को रंग दिया। ऐसा दहेज भी लौटा दिया जाता जिसमें विदेशी सामान हो, उसमें भी केवल देशी चीजें स्वीकार की जाती थी। पंडित ऐसी शादी करवाने से इंकार कर देते थे जहाँ विदेशी सामान का उपयोग होता था। मेहमान भी ऐसे समारोहों में नहीं जाते थे जहाँ विदेशी नमक या षक्कर का उपयोग होता था।’’
 स्वदेशी आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ‘‘आत्म-शक्ति’’ पर जोर दिया गया था। आत्म शक्ति का अर्थ है - राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्म विश्वास की घोषणा। आर्थिक क्षेत्र में इससे आषय था स्वदेशी उद्योगों की स्थापना। इसी दौर में कई कपड़ा मिलें, साबुन व माचिस की फैक्ट्रीयाँ, हस्तशिल्प व बुनकर उद्योग, राष्ट्रीय बैंक और इंश्योरंस कम्पनियाँ खोली गई। आचार्य पी. सी. राय ने प्रसिद्ध बंगाली केमिकल नाम से स्वदेशी स्टोर्स खोले। यहाँ तक कि रवीन्द्र नाथ टैगौर ने भी स्वदेशी स्टोर्स खोलने में मदद की।
स्वदेशी आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ‘‘आत्म-शक्ति’’ पर जोर दिया गया था। आत्म शक्ति का अर्थ है - राष्ट्रीय गरिमा, सम्मान और आत्म विश्वास की घोषणा। आर्थिक क्षेत्र में इससे आषय था स्वदेशी उद्योगों की स्थापना। इसी दौर में कई कपड़ा मिलें, साबुन व माचिस की फैक्ट्रीयाँ, हस्तशिल्प व बुनकर उद्योग, राष्ट्रीय बैंक और इंश्योरंस कम्पनियाँ खोली गई। आचार्य पी. सी. राय ने प्रसिद्ध बंगाली केमिकल नाम से स्वदेशी स्टोर्स खोले। यहाँ तक कि रवीन्द्र नाथ टैगौर ने भी स्वदेशी स्टोर्स खोलने में मदद की।
स्वदेशी आन्दोलन के कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिणाम निकले। राष्ट्रवादी गद्य, पद्य, व पत्रकारिता का विकास हुआ। इसी समय रवीन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकान्त सेन, सैय्यद अबु मोहम्मद और मुकुन्द दास जैसे कवियों द्वारा राष्ट्र भक्ति के गीत लिखे गये। इसी दौर में अन्य महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य हुआ राष्ट्रीय शिक्षा का विकास। राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्था खोला गया जहाँ साहित्यिक, तकनीकि या शारीरिक शिक्षा दी जा सके। राष्ट्रवादी समकालीन शिक्षा को गैर-राष्ट्रीय व अपर्याप्त मानते थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। एक राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसके प्राचार्य अरबिन्दो घोष थे, की भी स्थापना कलकत्ता में की गई।
C.10 छात्रों, महिलाओं और मुस्लिमों की भूमिका
बंगाल के छात्रों के द्वारा स्वदेशी आन्दोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया गया। उन्होने स्वदेशी आन्दोलन में भाग लेकर उसे गति दी तथा उन दुकानों को बंद करने में नेतृत्व किया जहाँ विदेशी वस्त्र बिकते थे। सरकार ने छात्र आंदोलन को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। उन स्कूलों व महाविद्यालयों की सूची बनाने का आदेश दिया गया जिनके छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे; उनके अनुदान, मदद और विशेषाधिकार वापस ले लिये गये, उनकी मान्यता रद्द की गई, उनके छात्रों पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने व सरकारी नौकरी हासिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले छात्रों के विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही की गई। उनमें से कई को विद्यालयों/महाविद्यालयों से निकाल दिया गया, गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा लाठियों से पीटा भी गया। हालांकि इससे छात्र आन्दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इसमें महिलाओं ने भी भागीदारी की। परम्परागत घरेलू महिलाओं ने रैलियों व धरनों में भाग लिया। तभी से महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की।
कई प्रमुख मुसलमानों जिनमें प्रसिद्ध वकील अब्दुल रसूल, प्रसिद्ध नेता लियाकत हुसैन और व्यापारी गज़नवी थे, ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी एक उग्र राष्ट्रवादी समूह से जुडे। ढाका के नवाब (जिन्हें सरकार द्वारा 14 लाख रू. का लोन दिया गया था) के नेतृत्व में कई उच्च मध्यमवर्गीय मुसलमानों ने उदासीन रहकर, इस आधार पर विभाजन का समर्थन किया कि, पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम बहुल इलाका होगा। इस साम्प्रदायिक दृष्टिकोण में ढाका के नवाब को सरकार का समर्थन भी मिला। लार्ड कर्जन ने, ढाका में एक भाषण में घोषित किया कि विभाजन के कारणोें में से एक यह भी था कि ‘‘पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को एक रखने से उनमें एकता होगी जो कि उन्होनें नवाबों के दौर के बाद खो दी है’’।
C.11 आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप
स्वदेशी और स्वराज आंदोलन भारत के अन्य प्रान्तों में भी फैल गया। बाॅम्बे, मद्रास और उत्तर भारत में बंगाल की एकता और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का समर्थन हुआ। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। उन्होनें शीघ्र ही महसूस किया की इतिहास में अपने किस्म के इस नये राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरूआत बंगाल में हो चुकी है। अब यह चुनौती और अवसर है कि इस लोकप्रिय आंदोलन को ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध नेतृत्व देकर पूरे भारत को एक सूत्र में बाँधा जाये।
C.12 उग्र राष्ट्रवाद का उदय
विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व शीघ्र ही उग्र राष्ट्रवादी हो गया। तिलक, विपिन चन्द्र पाल और अरबिंदो घोष इसके प्रमुख नेता थे। इसके कई कारण थे।
पहला, उदारवादियों का आंदोलन असफल हो चुका था। यहा तक कि जाॅन मार्ले, जो एक उदारवादी राज्य सचिव थे, ने भी उदारवादी नेताओं के सामने घोषित कर दिया था कि विभाजन सही था और अब इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा, दोनों बंगाल सरकार, मुख्य तौर पर पूर्वी बंगाल सरकार ने हिन्दुओं और मुसलमानों को बांटने का सक्रिय प्रयास किया। हिन्दु मुस्लिम विभाजन के बीज़ इसी दौर में बोये गये। इसने राष्ट्रवादियों को उत्तेजित किया पर इन सब में महत्वपूर्ण यह सरकार की नकारात्मक राजनीति थी जिससे लोग उग्र क्रांतिकारी राजनीति की ओर बढ़ने लगे। विशेष तौर पर पूर्वी बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। छात्र आंदोलन पर प्रतिबंध का जिक्र किया ही जा चुका है। पूर्वी बंगाल में गलियों में वंदे मातरम् गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सामूहिक सभाएँ प्रतिबंधित कर दी गई।
प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया व स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरूद्ध मुकद्मे चलाकर उन्हें लम्बी अवधियों के लिए जेल भेज दिया गया। कई छात्रों को शारीरिक यातनाएं भी दी गई। 1906 से 1909 तक बंगाल के न्यायालयों में लगभग 550 राजनैतिक केस दर्ज हुए। बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के विरूद्ध केस दर्ज कर प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। कई शहरों में मिलेट्री पुलिस स्थापित कर लोगों को दबाया गया। पुलिस बर्बरता का सबसे कुख्यात प्रदर्शन अप्रैल 1906 को बारिसाल में हुआ जहाँ शांतिपूर्ण बंगाल प्रांतीय सभा के प्रतिनिधियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। कई युवा प्रतिनिधि बुरे तरीके से पीटे गये और सभा को जबरन समाप्त घोषित किया गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
 दिसम्बर 12, 1908 में प्रसिद्ध नेता कृष्ण कुमार मित्रा और अश्विन कुमार दत्त सहित 9 बंगाली नेताओं को देश निकाला दे दिया गया। इससे पहले 1907 में लाला लाजपतराय और अजित सिंह को भी पंजाब में दंगों का दोशी पाते हुए देश निकाला दिया गया था। सन् 1900 में तिलक को भी गिरफ्तार कर छः वर्षों के लिए कठोर कारावास दिया गया था। मद्रास में चिदम्बरम् पिल्लई और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव को भी जेल हुई।
दिसम्बर 12, 1908 में प्रसिद्ध नेता कृष्ण कुमार मित्रा और अश्विन कुमार दत्त सहित 9 बंगाली नेताओं को देश निकाला दे दिया गया। इससे पहले 1907 में लाला लाजपतराय और अजित सिंह को भी पंजाब में दंगों का दोशी पाते हुए देश निकाला दिया गया था। सन् 1900 में तिलक को भी गिरफ्तार कर छः वर्षों के लिए कठोर कारावास दिया गया था। मद्रास में चिदम्बरम् पिल्लई और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव को भी जेल हुई।
जैसे ही उग्र राष्ट्रवादी परिदृश्य में आये, उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के साथ-साथ प्रतिरोध का भी नारा दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि सरकारी नौकरियों, अदालतों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों और नगर पालिकाओं और विधान परिशदों का बहिष्कार कर सरकार से असहयोग करें। जैसा कि अरविंदो घोष ने कहा - ‘‘इन परिस्थितियों में शासन करना असंभव होगा’’। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन को एक जन आंदोलन में बदलने का प्रयास किया और विदेशी शासन से स्वतंत्रता का नारा दिया। अरविंदो घोष से खुले रूप से घोषणा कि, ‘‘राजनैतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र के प्राण हैं’’। इस प्रकार बंगाल के विभाजन का प्रश्न पीछे छूटकर भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा प्रमुख हो गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने आत्मबलिदान का भी आव्हान किया जिसके बिना किसी उच्च लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता था।
 यह भी उल्लेखनीय है कि उग्र राष्ट्रवादी भी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल हो गये। वे जनता को प्रभावी नेतृत्व या प्रभावी संगठन देने में सफल नहीं हो सके। उन्होने जनता को जागृत किया पर वे यह नहीं जानते थे कि इस उर्जा का राष्ट्रीय संघर्ष के लिए कैसे उपयोग किया जाये। प्रतिरोध और असहयोग केवल विचार ही रहे, वे भारत के आम लोगों और किसानों तक नहीं पहुंच सके। उनका आंदोलन केवल शहरी निम्न और मध्यम वर्ग तथा जमीदारों तक ही सीमित रहा। 1908 तक वे राजनैतिक रूप से सुप्त हो गये। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें कुचलने में बड़े हद तक सफल रही। उनका आंदोलन तिलक की गिरफ्तारी, विपिन चन्द्र पाल और अरविंदो घोष के सक्रिय राजनैतिक जीवन से निवृत्ति के साथ समाप्त हो गया।
यह भी उल्लेखनीय है कि उग्र राष्ट्रवादी भी जनता को सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल हो गये। वे जनता को प्रभावी नेतृत्व या प्रभावी संगठन देने में सफल नहीं हो सके। उन्होने जनता को जागृत किया पर वे यह नहीं जानते थे कि इस उर्जा का राष्ट्रीय संघर्ष के लिए कैसे उपयोग किया जाये। प्रतिरोध और असहयोग केवल विचार ही रहे, वे भारत के आम लोगों और किसानों तक नहीं पहुंच सके। उनका आंदोलन केवल शहरी निम्न और मध्यम वर्ग तथा जमीदारों तक ही सीमित रहा। 1908 तक वे राजनैतिक रूप से सुप्त हो गये। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें कुचलने में बड़े हद तक सफल रही। उनका आंदोलन तिलक की गिरफ्तारी, विपिन चन्द्र पाल और अरविंदो घोष के सक्रिय राजनैतिक जीवन से निवृत्ति के साथ समाप्त हो गया।  किन्तु राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार थमा नहीं था। जनता को शताब्दियों की नींद से जगाया जा चुका था। उन्होनें राजनेति में भय रहित होना सीख लिया था। उन्होनें आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे सामूहिक राजनैतिक कार्य में आगे बढ़ना सीखा था। जनता एक नये आंदोलन के इंतजार में थी। इससे भी ज्यादा उस अनुभव से उन्होनें कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। गांधीजी ने लिखा कि ‘‘विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति से सहारा देना होगा। भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए विभाजन विरोधी यह आंदोलन एक नील का पत्थर था। बाद का राष्ट्रीय आंदोलन इसके अनुभवों से बहुत लाभान्वित होने वाला था।
किन्तु राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार थमा नहीं था। जनता को शताब्दियों की नींद से जगाया जा चुका था। उन्होनें राजनेति में भय रहित होना सीख लिया था। उन्होनें आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे सामूहिक राजनैतिक कार्य में आगे बढ़ना सीखा था। जनता एक नये आंदोलन के इंतजार में थी। इससे भी ज्यादा उस अनुभव से उन्होनें कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। गांधीजी ने लिखा कि ‘‘विभाजन के बाद लोगों ने देखा कि याचिका को शक्ति से सहारा देना होगा। भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए विभाजन विरोधी यह आंदोलन एक नील का पत्थर था। बाद का राष्ट्रीय आंदोलन इसके अनुभवों से बहुत लाभान्वित होने वाला था।C.13 क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय

सरकारी दमन और नेताओं द्वारा सकारात्मक नेतृत्व देने में असफल होने के कारण लोग अन्ततः उग्र व क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़े। बंगाल के युवाओं को जब शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रतिरोध के सारे रास्ते बंद मिले तो वे हिंसा की ओर मुड़ने लगे। उन्हें अब विश्वास नहीं रह गया था कि निष्क्रिय प्रतिरोध से राष्ट्रवादी उद्देश्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होने सोचा कि अंग्रेजों को देश से निकालना ही होगा। जैसा कि बारिसाल सभा के बाद 22 अप्रैल, 1906 को अपने अंक में युगान्तर ने लिखा कि: ‘‘समस्या का उपचार लोगों के पास ही हैं। भारत के 30 करोड़ लोगों को अपनी 60 करोड़ भुजाएं उठाकर इस दमन का विरोध करना ही होगा। शक्ति को ताकत के द्वारा ही रोका जा सकता है’’।
 किन्तु युवा क्रांतिकारियों ने जनक्रांति लाने की कोशिश नहीं की। इसके बदले उन्होनें आयरिश आतंकवादियों या रूसी क्रांतिकारियों की नकल की, जिसमें सीधे तौर पर अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना था। इसकी शुरूआत, 1897 में तब हुई जब चापेकर भाईयों ने दो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की पूना में हत्या कर दी। 1904 में वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का गठन किया। 1905 के बाद कुछ समाचार पत्रों ने भी क्रांतिकारियों का पक्ष लेना शुरू किया। उनमें से प्रमुख ‘‘संध्या’’ और ‘‘युगान्तर’’ बंगाल के तथा ‘‘काल’’ महाराष्ट्र से थे।
किन्तु युवा क्रांतिकारियों ने जनक्रांति लाने की कोशिश नहीं की। इसके बदले उन्होनें आयरिश आतंकवादियों या रूसी क्रांतिकारियों की नकल की, जिसमें सीधे तौर पर अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना था। इसकी शुरूआत, 1897 में तब हुई जब चापेकर भाईयों ने दो अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की पूना में हत्या कर दी। 1904 में वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का गठन किया। 1905 के बाद कुछ समाचार पत्रों ने भी क्रांतिकारियों का पक्ष लेना शुरू किया। उनमें से प्रमुख ‘‘संध्या’’ और ‘‘युगान्तर’’ बंगाल के तथा ‘‘काल’’ महाराष्ट्र से थे।
दिसम्बर 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास किया गया और अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक घोड़ा-गाड़ी पर बम फेंका जिसे वे मुजफ्फरपुर के एक कुख्यात जज किंग्सफोर्ड की समझ रहे थे। प्रफुल्ल चाकी ने तो स्वयं को गोली मार ली जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। कई क्रांतिकारियों ने इस दौर में गुप्त संगठनों की स्थापना की। इनमें से अनुषीलन समिति प्रमुख थी, जिसकी ढाका में ही 500 शाखाएँ थीं। शीघ्र क्रांतिकारी समाजवादी सारे देश में सक्रिय हो गये। उनके हौसले इतने बढ़ गये थे कि उन्होने वायसराय लाॅर्ड हार्डिंग पर भी बम फेंका जब वह एक सरकारी समारोह में हाथी की सवारी कर रहे थे। इस हमलें में वे घायल हो गये।
क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों के केन्द्र विदेशों में भी बनाये। इनमंे ष्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर और बर दयाल इंग्लैण्ड में जबकि मैडम कामा और अजीत सिंह यूरोप के प्रमुख नेता थे।
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी धीरे-धीरे असरहीन हो गया। वास्तव में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसे असफल होना ही था। यह जनता को गतिषील नहीं कर सका; वास्तव में जनता के बीच इसका कोई आधार नहीं था। किन्तु क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि एक इतिहासकार ने कहा है, ‘‘उन्होने हमें हमारे पुरुषार्थ से परिचित करवाया’’। उनकी वीरता व साहस के कारण, क्रांतिकारी देशवासियों के बीच लोकप्रिय हो गये यद्यपि राजनीतिक रूप से जागृत कई लोग उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
C.14 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1905-1914)

बंगाल विभाजन के प्रतिरोध आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पर गहरा प्रभाव पड़ा। काँग्रेस के सारे गुट विभाजन के विरोध में एक साथ खडे हो गये। 1905 के अधिवेशन में, कांग्रेस अध्यक्ष गोखले ने, विभाजन और लाॅर्ड कर्जन के तौर-तरीकों का जमकर विरोध किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी व बहिष्कार का भी समर्थन किया।
उदारवादी व उग्र राष्ट्रवादियों के तरीकों पर जनता में बहुत वाद-विवाद और असहमति थी। उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी व बहिष्कार को उपनिवेषिक सरकार के साथ पूर्णतः, और सम्पूर्ण देश में उपयोग करना चाहते थे। उदारवादी इसे केवल बंगाल में, वह भी केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे।
1906 में दोनों गुटों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर तनाव हो गया। अन्त में दादाभाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रवादी भी महान देशभक्त मानते थे, को अध्यक्ष चुना गया। दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में, खुले रूप से यह घोषणा कर राष्ट्रवादियों को उत्तेजित कर दिया कि ‘‘भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य ‘‘स्वराज’’ है।’’
किन्तु दोनों धड़ों के बीच का अन्तर पाटा नहीं जा सका। कई उदारवादी देशभक्त समय के साथ गति नहीं बना सके। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि भूतकाल में उनके द्वारा अपनाये गये सफल तरीके व दृष्टिकोण अब अपर्याप्त थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के इस नए मंच के साथ आगे नहीं बढ़ सके। उग्र राष्ट्रवादी किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दोनों ही धड़ों के बीच स्पष्ट विभाजन कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उभरकर सामने आया। कांग्रेस के विभिन्न पदों पर उदारवादी धड़ों का कब्जा हो गया और उग्र राष्ट्रवादी बाहर हो गये।
C.15 सूरत विभाजन
सूरत विभाजन आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1907 में जब उदारवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों के साथ कार्य करना छोड़ दिया तब यह विभाजन हुआ। विभाजन के कई कारण थे। उदारवादियों (नरम दल) का काँग्रेस पर शुरू से ही नियंत्रण था। उनके सोचने व कार्य करने का अपना तरीका था जो कि युवा पीढ़ी को स्वीकार नहीं था। युवा अधीर थे और उन्हें उदारवादियों का देश का नेतृत्व करने का तरीका पसंद नहीं था। अतः विभाजन होना ही था।
उदारवादियों (नरम दल) और उग्र राष्ट्रवादियों (गरम दल) के बीच विभाजन का मूल कारण, अंग्रेज शासन के प्रति वफादारी को लेकर था। उदारवादी अंग्रेजी राज के प्रति वफादारी में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि भारत में अंग्रेजी राज भारत की जनता के हित में था। दूसरी ओर कट्टरपंथी ब्रिटिश राज को श्राप मानते थे और अंग्रेज शासन के प्रति वफादारी का कोई कारण नहीं मानते थे।
वास्तव में दोनों ने ही अंतिम उद्देश्य पर ध्यान दिया और दोनों के ही अंतिम ध्येय में अंतर था। उदारवादी, समझदारी और समझौते की नीति पर विश्वास करते थे। वे ब्रिटिश संसद द्वारा समय-समय पर दी गई रियायतों से संतुष्ट थे, जबकि गरम दल के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनकी नजर में ‘‘स्वराज्य’’ ही समस्या का हल था। नरम दल के लोग केवल संवैधानिक तौर तरीकों पर विश्वास करते थे और ऐसी राह चुनते थे जिसमें कोई हिंसा न हो। वे तार्किक व भावुक आव्हानों, मामलों का स्पष्ट प्रतिनिधित्व, तथ्यों को दृढ़तापूर्वक रखना, तर्क और याचिका जैसे साधनों पर विश्वास रखते थे। उदारवादी असहयोग या निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधनों के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होनें स्वदेशी के कार्यक्रमों को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे बहिष्कार को आक्रामक कार्य मानते थे, जिससे दुर्भावना पैदा होती थी। दूसरी ओर गरम दल के लोग विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल तर्क, नैतिकता, दया से नहीं बल्कि शक्तिशाली आंदोलन से हो सकता है।
 नरम दल और गरम दल में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर उनकी कार्यप्रणाली का था। उदारवादी अपनी सफलता के लिए अंग्रेजों की सहानुभूति व इच्छा पर निर्भर थे। कट्टरपंथियों ने ऐसी कार्यप्रणाली को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत की जनता ही उसके भाग्य की निर्माता है न कि कोई विदेशी शक्ति। उदारवादी मानते थे कि भारत की जनता अभी स्वराज्य के योग्य नहीं थी, जबकि गरम दल के लोग मानते थे कि भारतीय ‘‘स्वराज्य’’ के योग्य हैं और इसे जनता की अयोग्यता के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। उदारवादी मानते थे कि वे जो माँगेगे, उन्हें बिना किसी कष्ट के आसानी से मिल जायेगा। गरम दल (कट्टरपंथी) के लोगों का मानना था कि भारत की मुक्ति कष्ट और आत्म-बलिदान के बिना संभव नहीं है।
नरम दल और गरम दल में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर उनकी कार्यप्रणाली का था। उदारवादी अपनी सफलता के लिए अंग्रेजों की सहानुभूति व इच्छा पर निर्भर थे। कट्टरपंथियों ने ऐसी कार्यप्रणाली को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत की जनता ही उसके भाग्य की निर्माता है न कि कोई विदेशी शक्ति। उदारवादी मानते थे कि भारत की जनता अभी स्वराज्य के योग्य नहीं थी, जबकि गरम दल के लोग मानते थे कि भारतीय ‘‘स्वराज्य’’ के योग्य हैं और इसे जनता की अयोग्यता के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। उदारवादी मानते थे कि वे जो माँगेगे, उन्हें बिना किसी कष्ट के आसानी से मिल जायेगा। गरम दल (कट्टरपंथी) के लोगों का मानना था कि भारत की मुक्ति कष्ट और आत्म-बलिदान के बिना संभव नहीं है।
इन अन्तरों के आधार पर, गरम दल व नरम दल के बीच टकराव था जो अन्ततः विभाजन की ओर ले गया। इससे इंकार नहीं है कि उदारवादी भी बंगाल विभाजन के उतने ही तीव्र विरोधी थे जितने की उग्र राष्ट्रवादी, तो भी उनकी अपनी सीमाएँ थी जिसके परे वे नहीं जा सकते थे। कांग्रेस ने 1906 में स्वदेशी, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया किन्तु उसे उदारवादियों का विरोध सहना पड़ा। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो कुछ हुआ उसे उदारवादियों ने अपनी सहमति नहीं दी और 1907 के सूरत अधिवेशन में उसे बदलने की कोशिश की। उग्र राष्ट्रवादी उन्हें ऐसा करने देने की अनुमति देने को तैयार नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में टकराव अवश्यंभावी था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy
C.16 सूरत विभाजन के परिणाम
सूरत विभाजन ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर कर दिया बल्कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन तक के लिए इसके प्रभाव को भी नष्ट कर दिया। अगले आठ सालों तक, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन अपने आप में विभाजित रहा, आधा संवैधानिक और आधा क्रांतिकारी। निश्चित रूप से यह अंग्रेजों को अच्छा ही लगा होगा!
[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]
FREE PT APP | CURRENT AFFAIRS Home All Posts Shrutis Power of 10 | CIVILS TAPASYA Home Tapasya Annual Prep - TAP GS-Study Mat. Exams Analyses Downloads | APTITUDE Power of Apti | TEST SERIES | CONTRIBUTE | TESTIMONIALS | PREMIUM PT GURUKUL | PRABODHAN Mastercourse | C.S.E. Self-Prep Online | SANDEEP SIR Site Youtube
नीचे दी गयी कमेंट्स थ्रेड में अपने विचार लिखें!















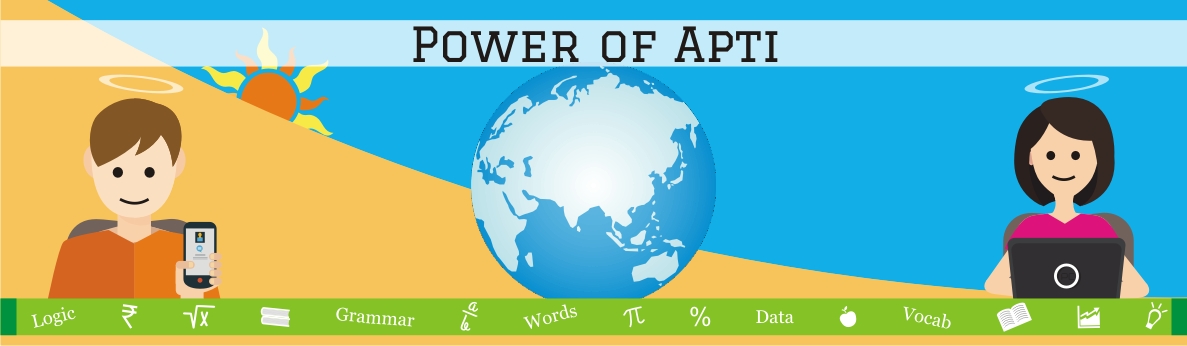













COMMENTS